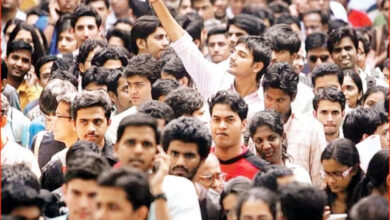अजय कुमार
उत्तर प्रदेश में अगले साल संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने गांव से लेकर शहर तक राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी भले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन गाँव-गाँव में चौपाल सजने लगी हैं। चाय की दुकानों, पंचायत चौपालों और खेतों के किनारों पर अब सिर्फ फसल और महंगाई की नहीं, बल्कि प्रधान बनने की रणनीतियों की बातें हो रही हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहे हैं। पंचायती चुनाव की महत्ता की बात की जाये तो पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य था ‘‘गाँव का शासन गाँव के हाथ में‘‘। एक तरफ गांव में चौपालें सज रही हैं तो दूसरी तरफ इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बदली हुई आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की सुगबुगाहट के चलते चुनाव लड़ने के इच्छुक कई नेताओं उम्मीदवारों की पेषानियों पर बल पड़ गये है। ऐसे इस लिये है क्योंकि हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट कहा था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया 2015 को आधार वर्ष मानकर लागू की जाये, इसी के साथ कोर्ट ने प्रदेष सरकार द्वारा जारी नई आरक्षण सूची को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले ने न केवल योगी सरकार की किरकिरी कराई बल्कि नई चुनौतियाँ भी खड़ी कीं हैं,वहीं हाईकोर्ट के फैसले ने ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गणित को भी पूरी तरह बदल दिया।
बहरहाल, पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लंबे समय से विवादास्पद रहा है। इस बार भी, जब सरकार ने नई आरक्षण नीति लागू करने की कोशिश की, तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नई आरक्षण नीति पारदर्शी नहीं है और यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी,जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि आरक्षण की व्यवस्था 2015 के आधार पर ही लागू की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले का असर ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों पर पड़ना तय है। कई उम्मीदवार, जो पहले से अपनी जीत की रणनीति बना चुके थे, अब नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गए। खास तौर पर, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण रहा। हाईकोर्ट के इस आदेश ने यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण का रोटेशन चक्रानुक्रम (रोटेशनल) तरीके से हो, जिससे हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
इसके बाद ही योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में 2015 के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का फैसला किया है। यह आयोग सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा और आरक्षण नीति को और मजबूत करने के लिए सुझाव देगा। इस कदम को सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत कुछ आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनाव को और जटिल बना सकती है। कोर्ट के पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ें फैसले ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित किया, बल्कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच भी एक नई बहस छेड़ दी। कई लोग इसे सामाजिक न्याय की जीत मान रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि बार-बार बदलती नीतियों से चुनावी प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ रही है। अब, पंचायती राज विभाग को नई आरक्षण सूची तैयार करने और कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की चुनौती है। ऐसे में चुनाव कराये जाने में देरी भी हो सकती है।
उधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नये सिरे से आरक्षण की व्यवस्था के बीच प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा 2026 के जनवरी और फरवरी माह में होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है और संबंधित विभागों को समय पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इन चुनावों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव की तिथियां देशभर के अन्य चुनावों और बोर्ड परीक्षाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दी जाएंगी। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव के लिये सबसे खास बात यह है कि यह संभवता यह चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराये जा सकते हैं। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि गाँव की ‘सरकार’ बनाने के लिये से प्रदेश की ‘राजधानी‘ लखनऊ तक में ‘पंचायतों‘ का दौर चल रहा है। सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व पूरी दमखम के साथ जुटा हुआ है क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजों से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिये भी ‘मैसेज’ निकलेगा।
एक समय था जब पंचायत चुनाव में राजनैतिक दल प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं लेते थे ,लेकिन अब करीब-करीब सभी राजनैतिक दल अपने प्रत्याशी उतारने से गुरेज नहीं करते हैं। यही वजह है कुछ राजनीतिक दल आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने पंचायत चुनावों में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने इसे 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल करार दिया है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। सुभासपा छड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और 15 जून तक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगी। वहीं अपना दल की नेत्री और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी पंचायत चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा करके बीजेपी खेमें में हलचल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां और राजनीतिक दलों की सक्रियता आगामी चुनावों के संकेत दे रही हैं।
गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव न केवल लोकतंत्र का सबसे निचला लेकिन सबसे प्रभावी स्तर है, बल्कि यह सामाजिक समीकरणों, जातीय राजनीति और स्थानीय विकास की बुनियाद भी तय करता है। हर गाँव में प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के लिए दावेदार तैयार हो रहे हैं। कुछ पुराने चेहरे एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं तो कुछ युवा नए उत्साह के साथ राजनीति में कदम रखने को तैयार हैं। इन चुनावों में जितनी भूमिका वादों और विकास की होती है, उतनी ही भूमिका जातीय समीकरणों, परंपराओं, स्थानीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों की भी होती है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव, विधानसभा या लोकसभा चुनाव से भी कहीं अधिक जटिल और व्यक्तिगत माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाँवों में पंचायत चुनावों का गणित अक्सर जातीय आधार पर तय होता है। जैसे ही आरक्षण सूची घोषित होती है, उम्मीदवारों की रणनीति बदल जाती है। जिस सीट पर पिछली बार किसी एक जाति का दबदबा था, इस बार अगर वह सीट आरक्षित हो जाए तो समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं।
इसके अलावा गाँव की राजनीति में ‘रिश्तेदारी की राजनीति’ भी गहरी होती है। किसी मोहल्ले या टोले से एक से अधिक प्रत्याशी आ जाएँ तो वोट कटने लगते हैं और तीसरा व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले उम्मीदवार एक-दूसरे को मनाने में लग जाते हैं कि ‘‘इस बार तुम नहीं, अगली बार सही।‘‘ आगामी पंचायत चुनाव के लिये इस बार यह भी देखा जा रहा है कि महिलाएं और युवा अधिक सक्रिय हैं। महिला आरक्षण के चलते कई महिलाएं अब केवल ‘‘नाममात्र की प्रधान‘‘ नहीं रहना चाहतीं, बल्कि खुद निर्णय लेने और गाँव के विकास में योगदान देने को तैयार हैं। वहीं युवा वर्ग भी परंपरागत राजनीति से हटकर नए मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं को चुनावी मंच पर ला रहा है। कई गाँवों में युवाओं के समूह ‘‘बदलाव मंच‘‘ या ‘‘युवा पंचायत‘‘ जैसे नामों से सक्रिय होकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं।जबकि पहले के समय में पंचायत चुनाव प्रचार घर-घर जाकर या चौपालों में बैठकर होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के जरिए अब प्रत्याशी अपनी छवि गाँव से बाहर तक भी बना रहे हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार पुराने तरीकों जैसे लाउडस्पीकर, पम्पलेट, बैनर और भंडारे का भी सहारा ले रहे हैं। हालांकि, इसके साथ ही ‘‘प्रलोभनों की राजनीति‘‘ भी सामने आ रही है। जबकि चुनाव से पहले शराब, पैसा, गिफ्ट और वादों का खेल भी गाँवों में देखा जा रहा है। यह न केवल चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करता है।
पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और हकीकत को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। चुनाव के दौरान लगभग हर प्रत्याशी गाँव के विकास की बात करता है जैसे पक्की सड़कें, साफ-सफाई, नाली व्यवस्था, बिजली, जल आपूर्ति और सरकारी योजनाओं की सही क्रियान्वयन। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अधिकांश वादे फाइलों में दबकर रह जाते हैं।परंतु अब स्थिति बदली है गाँवों के लोग अब पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं। वो अब सवाल करते हैं “पिछले पाँच साल में आपने क्या किया?”, “राशन योजना में घोटाला क्यों हुआ?”, “ग्राम निधि का सही उपयोग हुआ या नहीं?” इस तरह के सवाल प्रत्याशियों को अब झेलने पड़ रहे हैं।
पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पंचायत चुनाव के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने की तैयारियां जारी हैं। इसी के तहत पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों के वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया में जुटा है। जनसंख्या के अनुसार वार्डों का गठन किया जाएगा.1000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड, 2000 पर 11 वार्ड, 3000 पर 13 वार्ड और अधिकतम 15 वार्ड निर्धारित किए जाएंगे। चूंकि इस बार 512 ग्राम पंचायतें समाप्त हो रही हैं, ऐसे में वार्डों की संख्या में भी कमी आने की संभावना है। ग्राम पंचायतों की संख्या घटने से जिला पंचायत सदस्य सीटों में भी कुछ कमी का अनुमान है। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वार्ड गठन की प्रक्रिया 10 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। कुछ समय पूर्व पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के आंशिक पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की थी, जिसमें नए नगरीय निकायों के सृजन और सीमा विस्तार के चलते 512 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया, जबकि 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अब राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,694 रह गई है, जबकि 2021 में यह संख्या 58,195 थी।
आयोग राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके प्रभावों का समकालीन, सतत और अनुभवजन्य अध्ययन करेगा। आयोग उपलब्ध रिकॉर्ड, रिपोर्टों, सर्वेक्षणों और अन्य आंकड़ों का विश्लेषण कर यह पता लगाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों का अनुपात कितना है। साथ ही, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में अध्ययन करते हुए आयोग शासन को अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट तीन माह के भीतर या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपी जाएगी।