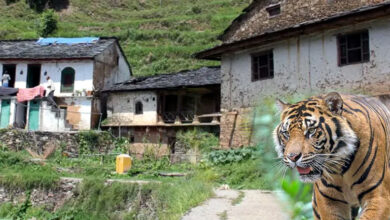रत्नज्योति दत्ता
नई दिल्ली – हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर आस्था गहरी है और पितृपक्ष के पखवाड़े में बिहार के पवित्र नगर गया में यह आस्था सबसे जीवंत रूप में प्रकट होती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु फल्गु नदी के तट पर एकत्र होकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और श्राद्धकर्म संपन्न करते हैं।
शास्त्रों के अनुसार यह अनुष्ठान आत्मा को मोक्ष दिलाता है और मानव जन्म में पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करता है। इस वर्ष भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे।
मैंने भी पखवाड़े के पहले दिन अपने माता-पिता का श्राद्धकर्म किया। मेरी पत्नी ने भी अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार से जुड़े अनुष्ठान पूरे किए। हमने इन कर्मों से अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
“यदि कोई गया में श्राद्धकर्म करता है, तो माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए आगे कोई और श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती,” स्थानीय पुजारी पवन लाल गुर्दा ने कहा।
पहले दिन भीड़ कम रही, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि आगे के दिनों में यहां जनसैलाब उमड़ पड़ता है। उत्तर-पूर्व भारत से आने वाले श्रद्धालु अपेक्षाकृत कम होते हैं, क्योंकि असम के ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में परिवार परंपरागत रूप से नदी तट पर ही पितृपक्ष के अनुष्ठान करते हैं। इसके बावजूद गया का अनुभव अद्वितीय है, जहां सहस्राब्दियों पुरानी परंपरा पवित्र फल्गु की भौगोलिकता से जुड़कर जीवंत होती है।
बौद्ध सर्किट की परंपरा
श्राद्धकर्म पूरा करने के बाद मैं बोधगया गया, जहां ढाई हजार वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान कर बुद्धत्व प्राप्त किया था।
सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाबोधि मंदिर आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थकेंद्र बना हुआ है। इसके चारों ओर थाईलैंड, भूटान और जापान जैसे देशों के मठ खड़े हैं, जो भारत और विश्व बौद्ध समुदाय के गहरे संबंध को दर्शाते हैं।
“यह आश्चर्य की बात है कि बौद्ध सर्किट तुर्की आक्रमणकारियों की निर्मम चोट से बच गया, लेकिन उनके घाव आज भी दिन की रोशनी में साफ दिखाई देते हैं,” पर्यटक गाइड सुजीत कुमार गुप्ता ने कहा।
इन घावों का सबसे बड़ा साक्ष्य नालंदा विश्वविद्यालय है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह विश्वविद्यालय पूरे एशिया से विद्वानों को आकर्षित करता था। 12वीं शताब्दी में जब मुहम्मद बख्तियार खिलजी की सेना ने विशाल पुस्तकालय में आग लगाई, तो वह छह महीने तक जलता रहा और अनगिनत पांडुलिपियाँ नष्ट हो गईं। खिलजी ने महाबोधि मंदिर समेत कई बौद्ध तीर्थस्थलों को भी भारी नुकसान पहुँचाया।
आज गया, बोधगया और नालंदा मिलकर ऐसा बौद्ध सर्किट बनाते हैं, जो सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत पाठ है—जहां हिंदू परंपरा का श्राद्धकर्म, बौद्ध धर्म का सार्वभौमिक संदेश और मध्यकालीन ध्वंस भारत की सभ्यता की अमर धारा को सामने लाते हैं।
ह्वेनसांग और भारत–चीन संबंध
हमने उस स्मारक परिसर का भी दौरा किया जो चीन के बौद्ध भिक्षु और विद्वान ह्वेनसांग (हुनसांग) को समर्पित है। उन्होंने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्ययन किया।
उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में नालंदा की भव्यता, विशाल पुस्तकालय और हजारों छात्रों का उल्लेख किया।
उनके विवरण आज भी नालंदा के ऐतिहासिक महत्व का प्रामाणिक दस्तावेज बने हुए हैं। यह स्मारक नालंदा के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और भारत–चीन की सभ्यतागत साझेदारी का प्रतीक है।
ह्वेनसांग का ऐतिहासिक दौरा याद दिलाता है कि कैसे ज्ञान और संस्कृति की साझेदारी ने सीमाओं से परे एक साझा परंपरा बनाई।
नई विश्व व्यवस्था का संदर्भ
वास्तव में ह्वेनसांग का नालंदा दौरा भारत–चीन संबंध की नींव बना। उनके अध्ययन और लेखन ने एशिया के इतिहास में सांस्कृतिक सेतु का निर्माण किया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी कायम है।
आधुनिक भू-राजनीति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एशियाई घनिष्ठता को रोकने की कोशिश की।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्वेनसांग के नालंदा संबंध की महत्ता पहचानी। उन्होंने इसे सभ्यतागत संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया और भारत को चीन व रूस के साथ और अधिक निकटता से जोड़ा।
हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। तीनों नेताओं ने मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था की माँग रखी, जिसमें ग्लोबल साउथ की आवाज़ और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दी जाए।
मोदी ने शी जिनपिंग से बातचीत में स्पष्ट कहा कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि विकास सहयोगी हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बिना भेदभाव की लड़ाई की आवश्यकता भी ज़ोर देकर उठाई।
नई विश्व व्यवस्था में भारत और चीन पश्चिमी प्रभुत्व के मुकाबले अपनी सामूहिक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं—और नालंदा का ऐतिहासिक प्रेरणा-स्रोत आज भी इस मार्ग में गूंजता है।
[लेखक दिल्ली स्थित पत्रकार हैं]