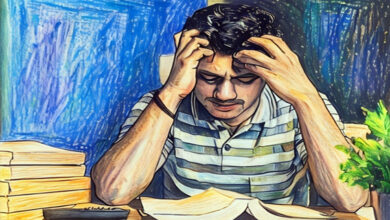अजेश कुमार
उत्तर प्रदेश की राजनीति का ज़िक्र आते ही सबसे पहले जो शब्द ज़हन में आता है, वह है जाति। यह राज्य केवल भौगोलिक रूप से विशाल नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी उतना ही जटिल है। जातियों की परतें यहाँ की राजनीति का सबसे अहम फैक्टर रही हैं। चुनावी रैलियों से लेकर मंत्रिमंडल की संरचना तक, सबकुछ जातीय गणित के हिसाब से तय होता रहा है। यही वजह है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर राज्य सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाया, तो यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर देने वाला कदम साबित हुआ।
16 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जाति के उल्लेख को पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक मंचों पर रोका जाए। अदालत ने साफ़ कहा कि यह प्रथा न केवल भेदभाव को बढ़ावा देती है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी ख़िलाफ़ है। अदालत ने अपने फैसले में डॉ. आंबेडकर को उद्धृत करते हुए जाति उन्मूलन के महत्व पर जोर दिया।
इसके बाद कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक विस्तृत आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि एफआईआर या गिरफ़्तारी मेमो में अभियुक्त की जाति नहीं लिखी जाएगी, बल्कि माता-पिता का नाम दर्ज किया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। साथ ही, राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का तर्क है कि इस तरह की रैलियां समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। मंडल कमीशन के लागू होने के बाद से जाति और धर्म की राजनीति का टकराव स्पष्ट दिखा। वी.पी. सिंह ने मंडल लागू किया तो बीजेपी ने उसकी काट कमंडल यानी राम मंदिर आंदोलन से निकाली। एक तरफ़ पिछड़े वर्गों को आरक्षण का आकर्षण था तो दूसरी तरफ़ धार्मिक ध्रुवीकरण। मंडल बनाम कमंडल की यह राजनीति दशकों तक चली। 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के साथ बीजेपी ने इसे नए रूप में ढाला, हिंदुत्व और सामाजिक इंजीनियरिंग का फ़ॉर्मूला। बीजेपी ने सवर्णों के साथ-साथ गैर-यादव ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई। यही रणनीति उसे 2017 और 2022 में विधानसभा चुनावों में बहुमत तक ले गई।
ओबीसी वर्ग में यादव, कुर्मी, शाक्य, कुशवाहा, निषाद, मौर्य जैसी जातियां हैं, जिनका राजनीतिक वजूद है। वहीं सवर्णों में ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य शामिल हैं। इन सबके बीच भाजपा ने संतुलन साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय के निर्विवाद नेता हैं। वहीं, अनुप्रिया पटेल (अपना दल) कुर्मी समुदाय को, और संजय निषाद (निषाद पार्टी) मछुआरा समाज को राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देते रहे हैं।सरकार के नए आदेश ने बीजेपी के सहयोगी दलों की राजनीति पर सीधा असर डाला है। निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे दल अपनी पहचान ही जातीय आधार पर बनाते आए हैं। संजय निषाद ने सरकार के इस फैसले पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि उत्पीड़ित जातियों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का हक़ होना चाहिए। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा भी अपने समुदाय के समर्थन से खड़ी हुई है। अपना दल खुद को “सबकी पार्टी” बताता है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यही है कि उसका आधार कुर्मी समाज है। आदेश लागू होने के बाद जातीय सम्मेलन करने की आज़ादी इन दलों के लिए सवाल खड़ा कर रही है।
समाजवादी पार्टी ने इस आदेश को अवसर बनाकर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? केवल रैलियों पर रोक लगाकर जातिवाद मिटेगा? सपा की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम-यादव समीकरण पर टिकी रही है। हाल के चुनावों में उसने “पीडीए” यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक का नारा देकर बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश की और लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। बसपा, जिसने दलितों को संगठित कर चार बार सत्ता हासिल की, अब काफी कमजोर हो चुकी है। मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाईं। कांग्रेस की हालत भी अलग नहीं है। कभी ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम गठजोड़ के दम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस अब हाशिए पर है।
बीजेपी खुद को ‘सबका साथ, सबका विकास’ की पार्टी बताती है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने जातीय प्रतीकों का इस्तेमाल खूब किया है। सुहेल देव, महाराजा बिजली पासी जैसे ऐतिहासिक पात्रों को भाजपा ने अपने अभियान में शामिल किया और समाज विशेष को जोड़ने में सफलता पाई। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बिजली पासी के नाम पर स्मारक बनाने का ऐलान किया। पासी समाज के लिए यह गौरव का क्षण था और भाजपा को एक और जातीय समूह को साधने का अवसर मिला।
कांग्रेस नेता अनिल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जातियों को छुपाकर वर्चस्ववादी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। उनका सवाल था कि क्या इस आदेश से दलितों पर अत्याचार बंद हो जाएंगे, या जाति के नाम पर होने वाली फर्ज़ी मुठभेड़ें थम जाएंगी? दूसरी ओर, विशेषज्ञ मानते हैं कि जातिगत सम्मेलन संविधान की भावना के ख़िलाफ़ हैं और विकास में बाधक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कोर्ट का आदेश जाति उन्मूलन की दिशा में सही कदम है, लेकिन जाति केवल कागज़ों से मिटाने से नहीं मिटेगी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में समय-समय पर अलग-अलग प्रयोग हुए हैं। 2007 में मायावती ने सर्व समाज का नारा देकर बहुमत हासिल किया। 2012 में अखिलेश यादव युवाओं और विकास की छवि के सहारे सत्ता में आए। 2017 और 2022 में बीजेपी हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत सत्ता में रही। अब 2027 की ओर नज़रें टिक गई हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले पर भरोसा कर रही है। भाजपा अपने सोशल इंजीनियरिंग और हिंदुत्व के सहारे मैदान में उतरेगी। कांग्रेस सपा के साथ है, जबकि मायावती अक्टूबर की रैली में अपने पत्ते खोलने वाली हैं।
इस आदेश से सीधा असर चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा। विपक्षी दलों के लिए जातीय सम्मेलन बंद हो जाएंगे, जबकि भाजपा अपने विकास और हिंदुत्व एजेंडे पर ज़ोर दे सकती है। इससे भाजपा को फायदा मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वह प्रतीकों, स्मारकों और सांस्कृतिक नैरेटिव के सहारे जातीय राजनीति साध सकती है। हालांकि, यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि जाति का असर कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर जाति केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान है। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रिश्ते-नातेदारी, और सामाजिक व्यवहार अब भी जाति से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में केवल रैलियों पर रोक से जातिवाद खत्म नहीं होगा।
कुल मिलाकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट और योगी सरकार का यह कदम ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह संविधान की उस मूल भावना को मजबूत करने की कोशिश है जिसमें नागरिक की पहचान धर्म और जाति से नहीं बल्कि इंसान और भारतीय होने से तय होती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह आदेश ज़मीनी हक़ीक़त बदल पाएगा? राजनीति में जाति का वजूद इतना गहरा है कि उसे केवल प्रशासनिक आदेश से मिटाना असंभव लगता है। हां, यह जरूर है कि जातीय रैलियों पर रोक से चुनावी रणनीतियों पर असर पड़ेगा और राजनीति का स्वरूप कुछ बदलेगा। लेकिन जातिवाद की जड़ें, जो समाज की परतों में गहराई तक फैली हैं, उन्हें खत्म करने के लिए कहीं ज़्यादा व्यापक सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की ज़रूरत होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जाति और धर्म के बीच झूलती रही है। अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह नया आदेश किसे नुकसान पहुंचाता है और किसे फायदा देता है। इतना तय है कि जाति की राजनीति भले सतह पर कुछ दब जाए, लेकिन उसकी छाया लंबे समय तक यूपी की राजनीति से हटने वाली नहीं है।