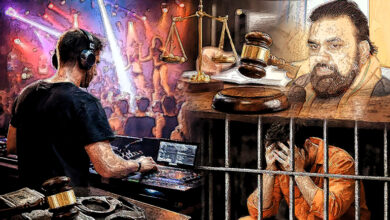जब करोड़ों भी दुल्हन नहीं दिला पाएँ: उत्तर भारत के लिंगानुपात की भयावह सच्चाई
उत्तर भारत में दुल्हन की तलाश में भटकते कुंवारे पुरुष कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि उस समाज की सामूहिक त्रासदी हैं जिसने वर्षों तक बेटियों को बोझ समझा। करोड़ों की संपत्ति, ऊँची नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा आज बेबस दिख रही है। यह संकट अचानक नहीं आया, बल्कि भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक सोच का स्वाभाविक परिणाम है। लिंगानुपात का यह असंतुलन केवल विवाह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर मानव तस्करी, ज़बरन विवाह और महिलाओं पर बढ़ती हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक संकटों को जन्म देगा। यह समय आँकड़ों से नहीं, सोच बदलने से समाधान खोजने का है।
डॉ. प्रियंका सौरभ
भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी संबंध नहीं होता, बल्कि वह समाज की सामूहिक चेतना, नैतिकता और सत्ता-संरचना का आईना भी होता है। लेकिन जब अख़बारों की सुर्ख़ियाँ यह बताने लगें कि करोड़ों की संपत्ति, लाखों की मासिक सैलरी और सरकारी नौकरी होने के बावजूद पुरुषों को दुल्हन नहीं मिल रही, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला व्यक्तिगत विफलता का नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और सभ्यतागत संकट का है। पंजाब और हरियाणा जैसे समृद्ध कहे जाने वाले राज्यों से आई यह सच्चाई किसी एक परिवार या वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि उस पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है, जिसने वर्षों तक बेटियों को जन्म से पहले ही मिटा दिया।
यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। यह किसी प्राकृतिक आपदा की तरह समाज पर नहीं टूटा, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से गढ़ा गया। अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग, दहेज की भूख, वंशवादी अहंकार और तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा ने मिलकर एक ऐसी ज़मीन तैयार की, जहाँ बेटियों का जन्म ही अपराध मान लिया गया। समाज ने यह मान लिया कि बेटा ही भविष्य है और बेटी बोझ। आज उसी सोच की कीमत समाज को सामूहिक रूप से चुकानी पड़ रही है।
सरकारी आँकड़े भले यह दावा करें कि लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, लेकिन विवाह के बाज़ार में दिखाई दे रही सच्चाई इन दावों की पोल खोल देती है। जब हज़ारों आवेदनों में 92 प्रतिशत पुरुष दुल्हन की तलाश में हों, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आँकड़े और ज़मीनी हकीकत के बीच एक गहरी खाई है। यह केवल संख्याओं का सवाल नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन का प्रश्न है। लिंगानुपात कोई साधारण जनसांख्यिकीय आँकड़ा नहीं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य का संकेतक होता है।
आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में 40 से 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके वे पुरुष विवाह के लिए दर-दर भटक रहे हैं, जिनके पास ज़मीन है, मकान है, गाड़ी है और सम्मानजनक नौकरी भी। वैवाहिक बैठकों में यह कहना कि “तलाक़शुदा चलेगी”, “एक बच्चा हो तो भी चलेगा”, किसी उदार सोच का नहीं, बल्कि गहरी हताशा का बयान है। यह वही समाज है जिसने कभी लड़की के रंग, रूप, कद और दहेज के आधार पर रिश्ते ठुकराए थे। आज वही समाज चयन से बाहर खड़ा है।
पितृसत्ता ने सदियों तक स्त्री को केवल एक वस्तु की तरह देखा—जिसे परखा जा सकता है, बदला जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। लेकिन आज वही पितृसत्ता अपने ही बनाए ढांचे में फँस गई है। यह उसकी ऐतिहासिक विफलता है कि उसने जिस व्यवस्था को अपने लाभ के लिए खड़ा किया, वही व्यवस्था अब उसके अस्तित्व पर सवाल बनकर खड़ी है। जिन इलाकों में भ्रूण हत्या सबसे अधिक हुई, वहीं आज विवाह संकट सबसे गहरा है। समाज ने सोचा था कि बेटियाँ कम होंगी तो बेटों की क़ीमत बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट—बेटियाँ कम हुईं और बेटों का भविष्य असुरक्षित हो गया।
इस स्थिति के लिए केवल परिवारों को दोष देना आसान है, लेकिन यह अधूरा सच होगा। राज्य, समाज और धर्म—तीनों इस संकट के सह-निर्माता हैं। प्रशासन ने लिंगानुपात को एक फ़ाइल में दर्ज होने वाला आँकड़ा समझा, संवेदनशील सामाजिक चेतावनी नहीं। राजनीति ने इसे कभी गंभीर चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि इससे तात्कालिक वोट नहीं मिलते। धर्म और जाति ने इसे संस्कार और परंपरा के नाम पर ढक दिया, मानो बेटी पैदा करना कोई अपराध हो।
‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे अभियान पोस्टरों, नारों और भाषणों तक सीमित रह गए। ज़मीनी स्तर पर सख़्ती, निरंतर सामाजिक संवाद और वैचारिक संघर्ष की जगह प्रचार ने ले ली। नतीजा यह हुआ कि योजनाएँ चलती रहीं और बेटियाँ घटती रहीं। समाज ने आँख मूँदकर यह मान लिया कि यह समस्या भविष्य की है, आज की नहीं। अब जब भविष्य दरवाज़े पर खड़ा है, तो घबराहट साफ़ दिखाई दे रही है।
आज दिखाई दे रहा यह विवाह संकट आने वाले सामाजिक विस्फोट का संकेत है। यदि यही स्थिति बनी रही, तो महिलाओं की ख़रीद-फरोख़्त, ज़बरन विवाह, मानव तस्करी और महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा जैसी घटनाएँ बढ़ेंगी। ये घटनाएँ किसी विकृत मानसिकता के अपवाद नहीं होंगी, बल्कि असंतुलित समाज का स्वाभाविक परिणाम होंगी। जब समाज में स्त्रियों की संख्या घटती है, तो उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ती, बल्कि उनका शोषण नए और अधिक ख़तरनाक रूपों में सामने आता है।
यह संकट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम स्त्री को अब भी केवल पत्नी, बहू और माँ की सीमित भूमिकाओं में ही बाँधकर देखेंगे, या उसे एक स्वतंत्र और बराबरी का नागरिक मानेंगे। जब तक बेटी को शिक्षा, संपत्ति में अधिकार, निर्णय की स्वतंत्रता और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी सामाजिक सुधार टिकाऊ नहीं हो सकता। यह समस्या कानून से ज़्यादा मानसिकता की है और मानसिकता बदलने के लिए साहसिक सामाजिक ईमानदारी चाहिए।
उत्तर भारत का यह विवाह संकट दरअसल एक आईना है—उस समाज के लिए, जिसने बेटियों को जन्म से पहले मिटा दिया और आज दुल्हन के लिए तरस रहा है। यह केवल अविवाहित पुरुषों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज की नैतिक हार है। जिस समाज ने स्त्री को बोझ समझा, वही समाज आज अपने ही बेटों का भविष्य ढो रहा है। अब भी समय है, लेकिन समाधान आँकड़ों, अभियानों और नारों से नहीं आएगा। इसकी शुरुआत सोच बदलने से ही होगी।