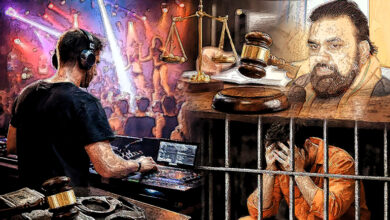डॉ. नीलम महेंद्र
हाल ही में एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि ब्रिटेन में परिवार के सदस्यों (दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे) या गैर-पारिवारिक सदस्यों के साथ एक छत के नीचे रहने का चलन बढ़ रहा है।
सिर्फ माता-पिता के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में सैकड़ों कम्युनिटी लिविंग ग्रुप्स बन गए हैं, जहाँ लोग सस्ते में रहते हैं और अकेलेपन से बचते हैं। वहां समाजशास्त्रियों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कम्युनिटी लिविंग या मल्टी-जेनरेशनल घरों में रहने वाले लोग अकेले या न्यूक्लियर फैमिली (एकल परिवार) में रहने वालों की तुलना में अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। नतीजन जो लोग अपने घर का खर्च उठा सकते हैं, वे भी अब कम्युनिटी लिविंग चुन रहे हैं, जिससे यह सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि वहां एक जीवनशैली का विकल्प बनता जा रहा है।
इसके विपरीत हम पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी की ओर भाग रहे हैं।आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास और वैश्विक पहचान के शोर में एक अत्यंत मौन लेकिन गहरी सामाजिक त्रासदी घट रही है और वो है संयुक्त परिवारों का विघटन।
विडंबना यह है कि जिस संयुक्त परिवार व्यवस्था को भारत ने पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर त्यागना शुरू किया, वही व्यवस्था आज पश्चिमी देशों में नए सामाजिक समाधान के रूप में अपनाई जा रही है।
भारत में संयुक्त परिवारों का विघटन केवल जीवन-शैली का बदलाव नहीं है बल्कि यह हमारे मूल सामाजिक दर्शन से विचलन है।
दरअसल भारत में संयुक्त परिवार कभी केवल साथ रहने की व्यवस्था मात्र नहीं रहा। अपितु यह एक ऐसा सांस्कृतिक सुरक्षा कवच था जहाँ बच्चे संस्कार सीखते थे, युवा जिम्मेदारी निभाते थे और बुज़ुर्ग सम्मान पाते थे। यह वह व्यवस्था थी जिसने बिना किसी मनोवैज्ञानिक परामर्श के पीढ़ियों को भावनात्मक रूप से संतुलित रखा। लेकिन आज वही व्यवस्था “स्पेस”, “प्राइवेसी” और “इंडिविजुअल फ्रीडम” जैसे शब्दों के नीचे दम तोड़ रही है।और जब परिवार टूटते हैं, तब केवल दीवारें अलग नहीं होतीं,तब संस्कार, संवेदनाएँ और सामाजिक संतुलन भी दरकने लगता है।
आंकड़े इस सामाजिक बदलाव की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019–21) के अनुसार भारत में लगभग 58.2% परिवार अब एकल (न्यूक्लियर) संरचना के हैं, जबकि संयुक्त परिवारों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है । यह स्पष्ट संकेत है कि संयुक्त परिवार अब अपवाद बनते जा रहे हैं।
शहरीकरण और रोजगार की मजबूरियाँ इस टूटन को और तेज़ कर रही हैं। शोध बताते हैं कि शहरी युवाओं में स्वतंत्रता और निजता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे संयुक्त परिवारों के साथ रहना “असुविधाजनक” समझा जाने लगा है । पर क्या सुविधा का अर्थ संवेदना का त्याग होना चाहिए, क्या स्वतंत्रता का अर्थ रिश्तों से मुक्ति है?
नतीजन आज भारत में परिवार छोटे हो रहे हैं और समस्याएँ बड़ी।
पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं, फिर भी मानसिक थकान बढ़ रही है।
बच्चे सुविधाओं से घिरे हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से असुरक्षित हैं।
और बुज़ुर्ग,जिनके अनुभव किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं,आज उपेक्षा और अकेलेपन के शिकार हैं।
जिस समाज में कभी बुज़ुर्ग परिवार का केंद्र होते थे, आज वहीं “ओल्ड एज होम” एक आवश्यक व्यवस्था बनती जा रही है। यह विकास नहीं, यह सामाजिक विफलता का संकेत है।
इसके उलट, यदि हम पश्चिमी देशों की ओर देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभरती है।
अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अब कम्युनिटी लिविंग, मल्टी-जेनरेशन होम्स और फैमिली सपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ सरकारें और समाज यह समझ चुके हैं कि अकेलापन सबसे महँगी बीमारी है,जिसका इलाज न दवाओं से होता है, न धन से।
जहाँ भारत संयुक्त परिवार से भाग रहा है, वहीं पश्चिम उसकी ओर आकर्षित ही नहीं हो रहा बल्कि उसे अपना भी रहा है।
यह विरोधाभास केवल सामाजिक नहीं, बल्कि बौद्धिक भी है।
हमने परंपरा को बोझ समझा, उन्होंने अनुभव को संपत्ति माना।
हमने बुज़ुर्गों को “डिपेंडेंसी” कहा, उन्होंने उन्हें मेंटल स्टेबिलिटी का आधार माना।
हम भूल गए कि संयुक्त परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी,सामूहिक उत्तरदायित्व।
बच्चे केवल माता-पिता के नहीं, पूरे परिवार के होते थे।
किसी एक के गिरने पर पूरा परिवार उसे संभाल लेता था।
आज इसके स्थान पर हमने संस्थागत विकल्प चुने हैं ,डे-केयर, ट्यूटर, काउंसलर और केयरटेकर।
पर सवाल यह है कि क्या भावनाओं की भरपाई सेवाओं से हो सकती है?
हमें यह समझ नहीं पाए कि संयुक्त परिवार व्यक्ति की पहचान को कुचलता नहीं था, (जैसा आज कहा जाता है) बल्कि वह उसे विस्तार देता था।
वहाँ व्यक्ति अकेला नहीं होता था क्योंकि
वहाँ असफलता साझा होती थी और सफलता सामूहिक।
आज भारतीय समाज जिस तनाव, अवसाद और पारिवारिक टूटन से जूझ रहा है, उसका बड़ा कारण यही है कि हमने रिश्तों की लागत को सुविधाओं के तराजू में तौलना शुरू कर दिया है।
हम भूल गए कि परिवार कोई अनुबंध नहीं होता, जिसे लाभ-हानि देखकर निभाया जाए।
अपितु वह एक उत्तरदायित्व होता है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।
यह भी सत्य है कि संयुक्त परिवारों में चुनौतियाँ थीं,मतभेद थे, टकराव थे, समझौते थे।
लेकिन क्या आधुनिक एकल परिवारों में टकराव नहीं हैं?
अंतर केवल इतना है कि वहाँ संभालने वाले अधिक थे,
और यहाँ झेलने वाला अकेला।
आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम अतीत में लौट जाएँ,
बल्कि यह समझने की है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
दरअसल सरकारें योजनाएँ बना सकती हैं,कानून सहारा दे सकते हैं,
लेकिन परिवारों को बचाने का काम केवल समाज कर सकता है।
यदि आज भी हमने इस टूटन को केवल “लाइफस्टाइल चेंज” कहकर नज़रअंदाज़ किया,
तो कल इसका परिणाम केवल सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय होगा।
क्योंकि इतिहास गवाह है कि
जिस समाज में परिवार कमजोर पड़ते हैं,
वहाँ राष्ट्र की नींव भी धीरे-धीरे दरकने लगती है।
अब भी समय है कि हम रुकें, सोचें और तय करें कि हमें अकेले मजबूत दिखना है या साथ मिलकर सच में मजबूत बनना है।
क्योंकि घर अलग-अलग हो सकते हैं,
लेकिन अगर दिल भी अलग हो जाएँ,
तो वह समाज नहीं, भीड़ बन जाती है।
डॉ. नीलम महेंद्र, लेखिका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य हैं।