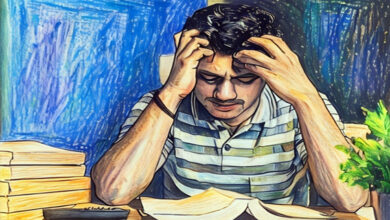सुनील कुमार महला
रंजना एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। समय पर स्कूल जाना, समय पर लौटना, बच्चों की कॉपियाँ जाँचना और घर की व्यवस्था संभालना-उसका जीवन एक अनुशासित लय में चलता था। उसके पति महेश एक कॉलेज में सेक्शन ऑफिसर थे। सीमित आमदनी थी, पर स्थिर। शहर के एक ठीक-ठाक मोहल्ले में उनका छोटा-सा घर था, जहाँ सुविधा थी, सादगी थी और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान। उनके दो बच्चे थे-नीलिमा और अरुण। नीलिमा समझदार और शांत स्वभाव की, जबकि अरुण चंचल, सवालों से भरा हुआ। दोनों बच्चों को रंजना ने हमेशा यही सिखाया था कि मेहनत से कमाया गया हर सुख सम्मान के साथ जीना चाहिए। अरुण के चाचाजी, यानी महेश के छोटे भाई, शहर के पास ही एक कस्बे में महिला प्रसाधन की दुकान चलाते थे। छोटी दुकान थी-चूड़ियाँ, बिंदी, कंघी, सिंदूर, नेल पॉलिश। दुकान से जैसे-तैसे घर चलता था। उनकी पत्नी आराध्या बिल्कुल देहाती थी। सादा पहनावा, कम बोलना, आँखों में हमेशा संकोच। वह गाँव में ही पली-बढ़ी थी, शहर में कभी आई नहीं थी। उस साल दिवाली नज़दीक थी। चाचाजी को किसी काम से शहर आना पड़ा, तो पहली बार आराध्या भी साथ चली आई। शहर की चमक-दमक, चौड़ी सड़कें, रोशनी से सजे बाज़ार-सब कुछ उसके लिए नया था। रंजना ने औपचारिकता में ही सही, उनका स्वागत अच्छे से किया। बच्चों को मिठाई दी, चाय नाश्ता कराया।आराध्या पूरे घर को चुपचाप देख रही थी-सोफ़ा, अलमारी, फ्रिज, टीवी। वह कुछ कहती नहीं थी, बस उसकी आँखें बहुत कुछ कह रही थीं। नीलिमा ने देखा कि उसकी चाची अपनी कलाई पर बँधी टूटी-सी काँच की चूड़ियों को बार-बार छू रही है। शाम को जब सब लोग बैठकर बात कर रहे थे, तभी आराध्या ने धीमी-सी आवाज़ में कहा, ‘भाभी… त्योहार आ रहा है… अगर हो सके तो… दो डिब्बी चूड़ियाँ…’ कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। महेश ने अख़बार से नज़र उठाई। रंजना की भौंहें तन गईं। ‘कौन-सी चूड़ियाँ?’ उसने सपाट स्वर में पूछा। ‘काँच की… वही बीस रुपये वाली…’ आराध्या ने जैसे हिम्मत जुटाकर कहा। रंजना के चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें मिठास नहीं थी। ‘आराध्या,’ उसने कहा, ‘कुछ डिमांड करने से पहले घर भी देख लेना चाहिए। हम कोई अमीर लोग नहीं हैं। हमारी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं।’ शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे छुपा भाव तीखा था।आराध्या का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। ‘जी भाभी…’और इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन चाचा-चाची वापस चले गए। जाते समय आराध्या ने बच्चों को सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। रंजना ने औपचारिक विदा दी। किसी ने नहीं देखा कि सीढ़ियाँ उतरते हुए आराध्या की आँखों से दो बूँद आँसू टपक पड़े। दिवाली आई। घर रोशनी से जगमगा उठा। रंजना ने अपने लिए नई चूड़ियाँ खरीदीं-थोड़ी महंगी, रंग-बिरंगी। पूजा के बाद जब उसने चूड़ियाँ पहनीं, तो अरुण ने अचानक पूछा, ‘माँ, चाची ने जो चूड़ियाँ माँगी थीं, वो आपने क्यों नहीं दी?’ रंजना झुँझला गई। ‘बच्चों को इन बातों से क्या मतलब!’ लेकिन अरुण चुप नहीं हुआ। ‘बीस रुपये की ही तो थीं…’ उस रात रंजना को नींद नहीं आई। उसे बार-बार आराध्या का झुका हुआ चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रही थी-क्या सचमुच वह इतनी गरीब नहीं थी कि बीस रुपये की चूड़ियाँ दे सके? या फिर उसे अपने ‘संपन्न’ होने का अहंकार था? कुछ दिन बाद खबर आई कि आराध्या गंभीर रूप से बीमार है। चाचाजी ने फोन पर रोते हुए बताया कि पैसे की कमी है। बिना देर किए रंजना और महेश गाँव पहुँचे। छोटे-से कच्चे घर में आराध्या खाट पर पड़ी थी। कलाई खाली थीं। आँखें धँसी हुईं, लेकिन चेहरा शांत। रंजना ने उसके पास बैठकर हाथ पकड़ा।
‘आराध्या… मैं…’ शब्द गले में अटक गए। आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ‘भाभी… चूड़ियाँ तो टूट जाती हैं… रिश्ते नहीं टूटने चाहिए…’ रंजना की आँखों से आँसू बह निकले। उसने अपने हाथ से चूड़ियाँ उतारीं और आराध्या की कलाई में पहना दीं। ‘मुझे माफ़ कर दो…’ आराध्या की आँखें बंद हो गईं। उसकी कलाई में चूड़ियों की धीमी-सी आवाज़ गूँज रही थी- जैसे किसी टूटे हुए अहंकार की अंतिम ध्वनि। उस दिन के बाद रंजना ने समझ लिया था-
संपन्नता घर की चीज़ों से नहीं, दिल की उदारता से आँकी जाती है।