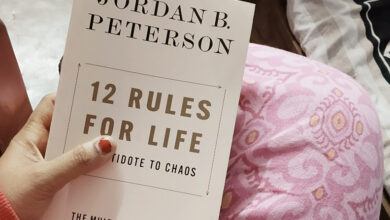मुनीष भाटिया
चिकित्सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से मानव जाति की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ रहा है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी से लेकर आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों तक, चिकित्सा विज्ञान ने मानव जीवन को न केवल लंबा किया है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया है। प्रारंभिक काल में चिकित्सा का मूल उद्देश्य रोगी को स्वस्थ करना और पीड़ा से मुक्ति दिलाना था, न कि लाभ कमाना। किन्तु वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र का स्वरूप तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई देता है। कथित रूप से फैलते मेडिसिन कॉर्पोरेट, बीमा कंपनियों और उनसे जुड़े व्यावसायिक हितों का दखल निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह सत्य है कि अनुसंधान जगत में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, नई-नई बीमारियों की पहचान हो रही है और उपचार के आधुनिक साधन विकसित हुए हैं। लेकिन इसके समानांतर यह तथ्य भी नकारा नहीं जा सकता कि रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। प्रश्न यह है कि यदि चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत हो रहा है, तो समाज पहले से अधिक बीमार क्यों होता जा रहा है?
आज बड़े-बड़े औद्योगिक घराने विशालकाय अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर “विश्वस्तरीय” या “अत्याधुनिक” कहा जाता है। इन अस्पतालों में जाँच के नाम पर अत्यधिक महंगे और कई बार अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा, जो कभी सेवा मानी जाती थी, अब एक सुनियोजित उद्योग का रूप ले चुकी है। अस्पतालों के आसपास व्यावसायिक और रिहायशी कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं, जिन्हें मेडिसिटी का नाम दिया जाता है—मानो बीमारी भी अब शहरी विकास का एक स्थायी घटक बन गई हो।विडंबना यह है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीमारियाँ कम नहीं हो रहीं।
कुछ दशक पहले जहाँ घरेलू उपचार या दो गोलियों से रोग नियंत्रित हो जाता था, वहीं आज दवाइयाँ किलो-आधा किलो के हिसाब से लिखी जा रही हैं। जीवनभर चलने वाली दवाइयाँ, निरंतर जाँच, और इलाज पर निर्भरता ने मानव को स्वस्थ से अधिक “स्थायी रोगी” बना दिया है।
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आज का रोगी उपचार के बाद स्वस्थ होकर व्यवस्था से बाहर नहीं निकलता, बल्कि एक स्थायी रोगी के रूप में उसी व्यवस्था से आजीवन जुड़ जाता है। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के नाम पर ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिन्हें “निरंतर” या “आजीवन” लेना अनिवार्य बताया जाता है। परिणामस्वरूप रोग समाप्त नहीं होता, केवल नियंत्रित किया जाता है—और नियंत्रण के नाम पर रोगी को दवा, जाँच और परामर्श की एक अंतहीन श्रृंखला में बाँध दिया जाता है।
स्वास्थ्य अब पूर्णता नहीं, बल्कि एक प्रबंधनीय स्थिति बन चुका है। यह प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक रोग-प्रतिरोधक क्षमता, पारंपरिक उपचार ज्ञान और आत्म-चिकित्सा की संभावनाओं को हाशिये पर धकेल देती है। इस प्रकार चिकित्सा का लक्ष्य स्वस्थ नागरिक नहीं, बल्कि लंबे समय तक उपभोक्ता बने रहने वाला स्थायी रोगी तैयार करना प्रतीत होता है। यह स्थिति केवल चिकित्सा विज्ञान की विफलता नहीं, बल्कि उसके व्यावसायीकरण की ओर भी इशारा करती है। जब लाभ स्वास्थ्य से बड़ा हो जाए, तब रोग का अंत नहीं, उसका विस्तार होता है। इसलिए यह प्रश्न केवल चिकित्सा पद्धति का नहीं, बल्कि नीति, नैतिकता और मानव मूल्यों का भी है। क्या चिकित्सा का उद्देश्य सचमुच रोगमुक्त समाज बनाना है, या फिर रोगों के माध्यम से एक अंतहीन बाज़ार खड़ा करना?
अंततः, यह विषय गंभीर आत्ममंथन की माँग करता है—चिकित्सा के वर्तमान मॉडल पर, उसके उद्देश्यों पर और उस दिशा पर, जिस ओर मानव स्वास्थ्य को ले जाया जा रहा है। क्योंकि यदि समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया, तो अस्पताल बढ़ते रहेंगे, दवाइयाँ बढ़ती रहेंगी, पर स्वस्थ मनुष्य दुर्लभ होता चला जाएगा।