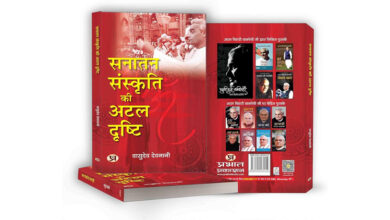चुपचाप मरते परिंदों की पुकार पर एक कविता
कोई पानी रख दे, कटोरे में भरकर,
मैं भी जी लूं ज़रा, इस तपते शहर में।
ना पुकार है मेरी किसी हैडलाइन में,
ना नाम मेरा किसी एनजीओ के बैनर में।
मैं चिड़िया हूं, गोरैया या बुलबुल,
सिर्फ परों में नहीं, सांसों में भी धूप है धुल।
कभी छज्जे पे बैठती थी,
अब छज्जा भी गरम तवा है।
पेड़ नहीं, छांव नहीं,
बस तारें हैं और धुएं की परछाई।
तुम्हारे एसी की ठंडक में
मेरी जान सूखती जाती है हर दोपहर।
तुम बिल जमा करते हो,
रील बनाते हो,
पर क्या एक बर्तन भर पानी रखना
इतना मुश्किल काम है?
मैं पूछती नहीं,
बस ताकती हूं,
कभी बालकनी, कभी खिड़की की जाली।
कभी किसी बुज़ुर्ग की मिट्टी की सुराही याद आती है।
मुझे मत बचाओ किसी बड़ी योजना से,
न किसी बजट, न किसी फंड से।
बस एक कोना दे दो —
जहां मेरी प्यास, मेरी जान बच सके।
इस गर्मी में जब तुम्हें भी लगने लगे कि सांसें भारी हैं,
तो एक बार मेरी ओर देखना…
मैं चुपचाप बैठी होऊंगी,
उस सूखे कटोरे के पास —
उम्मीद में कि
कोई पानी डाल दे तो मैं भी
चौंच भर पीलूं।
प्रियंका सौरभ