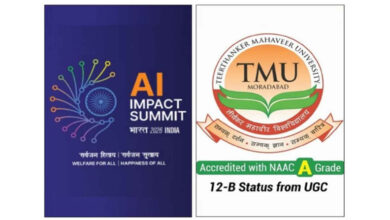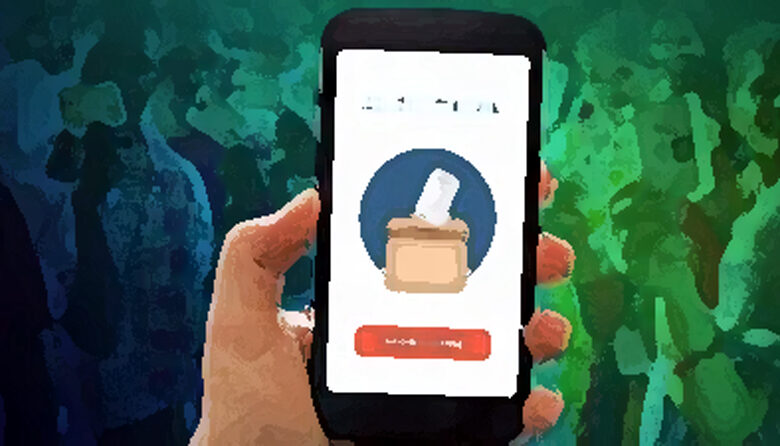
ई- वोटिंग ने रच दिया इतिहास
प्रमोद भार्गव
देष में मतदान के प्रति अरुचि प्रत्येक चुनाव में देखने में आती रही है। रोगग्रस्त या अन्य लाचारों को तो छोड़िए, उच्च षिक्षित एवं सक्षम कुलीन वर्ग मतदान के प्रति सबसे ज्यादा उदासीन रहता है। वैसे तो निर्वाचन आयोग मतदान का प्रतिषत और सुविधा के मतदान के लिए अनेक प्रयोग करता रहा है, लेकिन अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के उपचुनाव में पहली बार ई-वोटिंग का प्रयोग करके इतिहास रच दिया है। मोबाइल से मतदान की सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई, जो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट देने से मजबूर थे। तमाम मतदाता गांव और राज्य से बाहर होने के कारण मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन मोबाइल से ई-मतदान की सुविधा के चलते बिहार के इस चुनाव में 80.60 प्रतिशत और उपचुनाव में 58.38 प्रतिशत मतदाताओं ने मोबाइल के जरिए मतदान किया। पहली महिला ई-वोटर विभा कुमारी और पहले पुरुश मतदाता मुन्ना कुमार बने।
राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद ने मोबाइल से ई-मतदान कराए जाने की प्रेरणा यूरोपीए देष एस्टोनिया से ली। चूंकि अब ई-वोटिंग का सफल प्रयोग हो चुका है, इसलिए भविश्य में इसकी मांग बढ़ेगी। जो गर्भवती महिलाएं, बुर्जुग, विकलांग, असाध्य रोगों से ग्रसित और अपने मतदान स्थल से दूर रहने वाले लोग मतदान से वंचित रह जाते थे, उन्हें लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भागीदार बनने की आसान सुविधा मिल जाएगी। इस सुविधा से एक बड़ी समस्या का सामाधान बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हो जाएगा। चूंकि मतदान केंद्रों पर विभिन्न दलों का जमावड़ा नहीं होगा, इसलिए निश्पक्ष और षांतिपूर्ण मतदान की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मतदान की निजता भी प्रभावित नहीं होगी। इससे मतदान के प्रतिषत में आषातीत सुधार तो होगा ही, जातीय और सांप्रदायिक धु्रवीकरण की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएंगी। ई-वोटिंग का काम पूर्वी चंपारण जिले की नगर पंचायत पकड़ी दयाल के अलावा पटना, बक्सर, रोहतास, सारण और बांका में सी-डैक और एसईआर के जरिए किया गया था।
अब यह जरूरी लगता है कि जब पैसे के लेनदेन से लेकर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के काम ऑनलाइन या डिजिटल प्रणालियों से हो रहे हैं तो फिर ई-मतदान को भी जरूरी बनाया जाए। बिहार के उपचुनाव में मोबाइल एप से ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्रमाणित भी हो चुकी है। ई-वोटिंग को इसलिए भी अपनाया जाए, क्योंकि पूर्व से ही हमारे यहां पोस्टल वोटिंग का वैधानिक प्रावधान है। मतदान संपन्न कराने में जुटे कर्मचारी अपना वोट पोस्टल वोटिंग के जरिए ही देते हैं। अब कोई राजनीतिक दल और नेता यह बहाना नहीं बना सकता है कि अभी इंटरनेट या बिजली की सुविधा दुर्गम क्षेत्रों में नहीं है। एक बार बिजली भले ही प्रत्येक ग्राम में न हो, लेकिन सौर ऊर्जा से बिजली और मोबाइल टॉवर गांव-गांव पहुंच गए हैं। इनके जरिए इंटरनेट की सुविधा हासिल कराई जा रही है। सौर जैसी वैकल्पिक ऊर्जा दूर-दराज के ग्रामों में बिजली उपलब्ध करा रही है।
फिर भी किसी गांव में बिजली नहीं है तो वहां ईवीएम के जरिए मतदान कराया जाए। ई-वोटिंग को चरणबद्ध रूप में कराए जाने का सिलसिला जल्द से जल्द षुरू होता है तो लोकतंत्र में लोगों की उम्मीद से ज्यादा भागीदारी बढ़ती दिखाई देगी। हालांकि मोबाइल से ई-वोटिंग को लेकर कुछ नेता अभी से संदेह जताने लगे हैं। उनका कहना है कि मोबाइल एप पर पंजीकरण में कठिनाई आएगी। गांव के प्रभावी लोग दबाव बनाकर पक्षपातपूर्ण एवं फर्जी मतदान करा सकते है। भारत में फर्जी और दबाव से मतदान की अपवाद स्वरूप घटनाएं आज भी देखने में आ जाती हैं। ईवीएम से मतदान पर आज भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ईवीएम की साख पर ठोस प्रमाण कोई दल या इंजीनियर आज तक नहीं दे पाया है। ई-वोटिंग पूरे देष के लिए अपना ली जाती है तो चुनाव खर्च में तो कमी आएगी ही, तकनीक की सार्थकता भी पेष आएगी।
घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए ई-वोटिंग की जरूरत इसलिए है, क्योंकि बड़ी संख्या में देष के मतदाता मजदूरी, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी और अन्य काम-धंधों के लिए मूल निवास स्थल छोड़ जाते हैं। इसलिए वे चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। आयोग का कहना है कि 2019 के आम चुनाव में करीब 30 करोड़ यानी 67.4 प्रतिषत लोग इन्हीं कारणों के चलते अपने मत का उपयोग नहीं कर पाए थे। ऐसा लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में होता है। चुनाव विषेशज्ञों का तो यहां तक मानना है कि करीब 45 करोड़ लोग पलायन के चलते मतदान से वंचित हो जाते हैं। इसलिए लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि इन देषज प्रवासियों के मतदान का कोई व्यावहारिक उपाय निकाला जाना चाहिए। इस नजरिए से प्रवासियों के लिए ई-वोटिंग उपयोगी है।
हालांकि चुनाव सुधार की दृष्टि से चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले अर्थात दूरस्थ मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम (आरवीएस) तैयार किया हुआ है। इस मशीन की मदद से अब मूल मतदान स्थल से दूर रह रहे किसी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। यानी मतदान के लिए उन्हें अपने मूल निवास स्थल पर आने की जरूरत नहीं रह गई हैं। आयोग इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रषासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी आमंत्रित किए जाएंगे। चुनाव सुधार की दृश्टि से यह पहल अमल में आती है तो ऐतिहासिक होगी। नतीजतन उन 45 करोड़ लोगों को वोट डालने का अवसर मिलेगा, जो अपने घरों से दूर रहते हैं। यह उपाय मत-प्रतिषत बढ़ाने का भी काम करेगा। यानी जनप्रतिनिधियों का चुनाव अधिकतम मतदाताओं के वोट डालने से होगा, जो लोकतंत्र को पारदर्षी बनाने का काम करेगा। इस सिलसिले में आयोग ने दावा किया है कि यह मषीन त्रृटिहीन बनाई गई है, इसलिए मतदान निश्पक्ष होगा। हालांकि मतदान की इस प्रक्रिया को इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। आयोग फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहता है, जिससे इसके प्रयोग की निश्पक्षता स्पश्ट हो जाए। बाद में इसे पूरे देष में अनिवार्य बना दिया जाएगा। अनेक चुनाव विषेशज्ञ इस प्रणाली को एक क्रांतिकारी पहल मानकर चल रहे हैं।
देष में निसंदेह एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो अपना घर और षहर छोड़कर आजीविका के लिए दूसरे षहरों या राज्यों में रह रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवा हैं। हालांकि इनका कोई एकीकृत आंकड़ा देष और आयोग के पास नहीं है। फिर भी सब जानते है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता हैं। ये लोग नई जगह पहुंचने के बाद नया वोटर पंजीयन भी नहीं कराते हैं। नतीजतन मतदान से वंचित रहते हैं। इन्हें जहां रह रहे हैं, वहीं मतदान की सुविधा मिल जाए, इस नजरिए से आरवीएम की परिकल्पना की गई है। आईआईटी मद्रास की मदद से ‘मल्टी कॉन्स्टीचुएंसी रिमोट ईवीएम‘ के रूप में ऐसा मतदान उपकरण तैयार किया गया है, जो एक रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवासियों का मतदान कराने में सक्षम होगा। हालांकि आरवीएम के इस्तेमाल को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध जता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे मतदान के प्रति लोगों का भरोसा कम होगा। प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए आदर्श स्थिति यही है कि हरेक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस नाते 2005 में भाजपा के एक सांसद लोकसभा में ‘अनिवार्य मतदान’ संबंधी विधेयक लाए भी थे। लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस व अन्य दलों ने इस विधेयक के विरोध का कारण बताया था कि दबाव डालकर मतदान कराना संविधान की अवहेलना है। क्योंकि भारतीय संविधान में अब तक मतदान करना मतदाता का स्वैच्छिक अधिकार तो है, लेकिन वह इस कर्तव्य-पालन के लिए बाध्यकारी नहीं है। लिहाजा वह इस राष्ट्रीय दायित्व को गंभीरता से न लेते हुए, उदासीनता बरतता है। हमारे यहां आर्थिक रूप से संपन्न सुविधा भोगी जो तबका है, वह अनिवार्य मतदान को संविधान में दी निजी स्वतंत्रता में बाधा मानते हुए इसका मखौल उड़ाता है।
मतदान की अनिवार्यता अथवा ई-वोटिंग या आरवीएम से सुविधा का मतदान कथित अल्पसंख्यक व जातीय समूहों को ‘वोट बैंक’ की लाचारगी से भी छुटकारा दिलाएगी। राजनीतिक दलों को भी तुष्टिकरण की राजनीति से निजात मिलेगी। क्योंकि जब प्रवासियों को आरवीएम से मतदान की सुविधा मिल जाएगी तो किसी धर्म, जाति या क्षेत्र विशेष से जुड़े मतदाताओं की अहंमियत खत्म हो जाएगी। नतीजतन उनका संख्याबल जीत अथवा हार को प्रभावित नहीं कर पायेगा। लिहाजा सांप्रदायिक व जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की जरूरत नगण्य हो जाएगी। जब पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की छाया थी, तब वहां हुए विधानसभा चुनावों में 15 से लेकर 20 प्रतिशत मतदान से ही सरकारें बनती रही हैं। साफ है, यह स्थिति लोकतंत्र के लिए उचित नहीं रही। अतएव अधिकतम मतदान के हालात ई-वोटिंग एवं आरवीएम के इस्तेमाल से निर्मित होते हैं तो भारतीय राजनीति संविधान के उस सिद्धांत का पालन करने को विवश होगी, जो सामाजिक न्याय और समान अवसर की वकालात करता है।