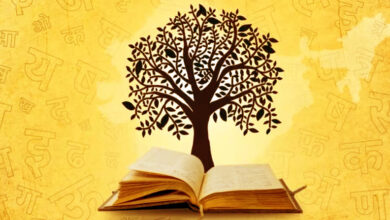प्रिंस अभिषेक
बिहार की राजनीति हमेशा से देश की सबसे गतिशील, जटिल और अप्रत्याशित राजनीति रही है। यहाँ चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों, जातीय संतुलन और राजनीतिक चालबाज़ियों का खेल भी होता है। त्योहारी माहौल में भी बिहार की जनता की चर्चा राजनीति से आगे नहीं बढ़ती, मानो राजनीति ही उनका सबसे बड़ा मनोरंजन हो। पिछले दो दशकों में बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति रहे हैं नीतीश कुमार और इस दौर में एक कहावत ने जन्म लिया- “पावर वहीं झुकती है, जहाँ नीतीश झुकते हैं।”
दरअसल, बिहार की राजनीति का सबसे रोचक पहलू यही है कि नीतीश कुमार जब जिस खेमे में जाते हैं, वही सत्ता के करीब पहुँच जाता है। यही वजह है कि भाजपा, जो आमतौर पर अपने सहयोगियों को हाशिए पर डाल देती है, बिहार में नीतीश के आगे झुकने पर मजबूर होती रही है। यही स्थिति कभी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ भी रही थी, जब वह नीतीश के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) यानी जदयू के साथ गठबंधन में थे। बिहार में गठबंधनों की राजनीति हमेशा से “सत्ता की कुंजी” रही है, और इस कुंजी के सबसे चतुर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उनके खिलाफ जो भी दल बोलता है, अंततः वही दल किसी न किसी समय उनके साथ हाथ मिला लेता है। 2017 में महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ गए नीतीश 2022 में फिर आरजेडी के साथ लौट आए। इसका कारण यही है कि बिहार में सत्ता प्राप्त करने का रास्ता नीतीश से होकर ही गुजरता है। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल रही हैं- जदयू के संगठनात्मक ढांचे में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब उतनी अटूट नहीं रही जितनी पहले थी।
नीतीश के राजनीतिक सफर की शुरुआत विकास और सुशासन के वादे से हुई थी। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, शिक्षा और सड़क सुधार पर व्यापक काम किया। 2006 में शुरू किया गया “स्कूल चलो अभियान” और लड़कियों को साइकिल वितरण जैसी योजनाओं ने शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाया। 2005 में जहाँ केवल 1.8 लाख लड़कियाँ 10वीं की परीक्षा में शामिल हुई थीं, वहीं अब यह संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है। उन्होंने महिलाओं को घर और पानी की सुविधा देने की भी कोशिश की, हालांकि यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। लेकिन इन पहलों ने उन्हें ‘सुशासन बाबू’ की पहचान दिलाई।
हालाँकि समय के साथ परिस्थितियाँ बदलीं। तीसरे और चौथे कार्यकाल में नीतीश कुमार के शासन पर विकास की गति धीमी पड़ी। पलायन, बेरोज़गारी और उद्योगों की कमी जैसी समस्याएँ फिर उभर आईं। अब नीतीश का प्रशासन अक्सर विकास की बजाय गठबंधन राजनीति में उलझा दिखता है। एक समय जिनके कामकाज को बिहार की जनता मिसाल के रूप में देखती थी, अब वही जनता उन्हें असमंजस और सत्ता-लोलुपता के प्रतीक के रूप में देखने लगी है।
इस बार नीतीश को कई मोर्चों से चुनौती मिल रही है। उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और पार्टी के भीतर असंतोष भी बढ़ा है। जदयू का जनाधार धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है और आरजेडी या भाजपा में से किसी एक की सहायता के बिना उनके लिए सत्ता में बने रहना कठिन हो गया है। यही वजह है कि नीतीश सरकार ने हाल ही में महिलाओं को ₹10,000 की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की और अनेक रियायतें घोषित की, ताकि जनसमर्थन दोबारा हासिल किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन “दोलों” और रियायतों से जनता का रुझान वास्तव में बदलेगा?
दूसरी ओर, तेजस्वी यादव का राजनीतिक प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है। पिछली विधानसभा चुनाव में महागठबंधन केवल 16,825 वोटों से हारा था, जो एक बेहद मामूली अंतर है। तेजस्वी की लोकप्रियता युवाओं और बेरोज़गारों के बीच काफ़ी बढ़ी है। उन्हें कांग्रेस और वामपंथी दलों का भी समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेजस्वी को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पारिवारिक महत्वाकांक्षाएँ और सहयोगी दलों के बीच सीट बँटवारे को लेकर असहमति महागठबंधन के लिए चुनौती बन गई है।
महागठबंधन की वर्तमान स्थिति थोड़ी जटिल है। सीट शेयरिंग को लेकर तकरार हमेशा की तरह जारी है, लेकिन अंततः सभी दल एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वहीं, नए मतदाता आंकड़ों ने समीकरणों को और पेचीदा बना दिया है। हाल ही में चुनाव आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 69 लाख पुराने मतदाता हटाए गए हैं और 21 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जो किसी भी दल के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
इसी बीच, प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी भी इस चुनावी परिदृश्य में नया आयाम जोड़ रही है। प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान चुनावी रणनीतिकार के रूप में बनाई थी, लेकिन अब वे एक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पदयात्राएँ, जन संवाद और सीधे जनता से जुड़ने की शैली ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। वे भाजपा, जदयू और आरजेडी- सभी पर तीखे प्रहार कर रहे हैं और अपने समर्थक वर्ग को बढ़ा रहे हैं। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि वे सरकार बनाएँगे या “किंगमेकर” की भूमिका में रहेंगे।
भाजपा की स्थिति भी इस बार उतनी आसान नहीं है। संगठनात्मक रूप से यह सबसे मजबूत पार्टी है, परंतु बिहार में उसके पास कोई दमदार स्थानीय चेहरा नहीं है। पिछली बार भाजपा ने जदयू से दोगुनी सीटें जीतीं, फिर भी उसे मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। इसने उसके कैडर में असंतोष पैदा किया। भाजपा के सहयोगी जैसे चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उसे मजबूती तो देते हैं, लेकिन जातीय गणित और स्थानीय असंतुलन भाजपा के लिए भी चुनौती बना हुआ है। बिहार की राजनीति में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नीतीश कुमार किसके साथ जाते हैं- भाजपा या आरजेडी। उनका यह निर्णय ही तय करेगा कि राज्य में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी। हालांकि इस बार उनके पास पहले जैसी राजनीतिक पूँजी नहीं है। जनता विकास, रोज़गार और स्थिरता चाहती है, और लगातार पलटते गठबंधन उसकी थकान को बढ़ा रहे हैं।
यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के चुनावी नाटक का “फाइनल एक्ट” अभी बाकी है। सत्ता के इस रंगमंच पर सभी पात्र अपनी भूमिका निभा रहे हैं- कोई नायक बनने की कोशिश में है तो कोई पर्दे के पीछे से खेल रच रहा है। लेकिन आख़िरी सीन तभी तय होगा जब मतदान के बाद जनता का निर्णय सामने आएगा। तब ही यह साफ़ होगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से “किंगमेकर” बनेंगे या इस बार बिहार किसी नए नेता के हाथों अपनी राजनीतिक पटकथा लिखेगा। बिहार एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ा है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राज्य की दिशा तय करने का चुनाव है। जातीय समीकरणों, राजनीतिक गठबंधनों और विकास के वादों के बीच बिहार की जनता को यह तय करना होगा कि वह स्थिरता चाहती है या बदलाव। और जैसा कि हमेशा होता आया है- बिहार की राजनीति का अंत तब तक तय नहीं होता जब तक अंतिम वोट की गिनती पूरी न हो जाए।