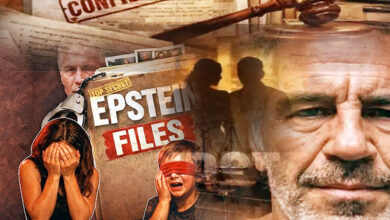नृपेन्द्र अभिषेक नृप
साहित्य साधना में डूबा साधक साहित्य सागर से भिन्न भिन्न प्रकार के मोती निकाल के लाता है। उस मोती का समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है यह उस मोती को पढ़ने समझने व परखने से पता चलता है। ऐसे ही एक साहित्य सागर से ‘कहीं कुछ अनकहा’ मोती निकाल लाए हैं ध्रुव गुप्त। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे ध्रुव गुप्त की पुस्तक ‘कहीं कुछ अनकहा’ उनकी 93 प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है। इनमें हर तरह की कविताएँ शामिल हैं। कवि के भीतर सबसे ज्यादा प्रकृति प्रेम भरा हुआ है। उनकी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न पहलूओं को छूने की कोशिश है। इसके अलावे प्रेम के विभिन्न रंगो को कवि ने इस किताब में संजोया है जो अंतर्मन को छूती हैं।
पुस्तक की पहली कविता बची रहे प्रतीक्षा में वृक्ष, बारिश, हवा, नदी, जंगल आदि को बचाए रखने के आग्रह के बीच दिल में सुकून व होठों पर मुस्कान के साथ किसी के आने की प्रतीक्षा की बात है। यह जीवन को एक नई उम्मीद देने के तरफ इशारा है। कवि ने उस फूल को महसूस किया है जिसको समाज कोई महत्व नहीं देता। मसलन बेहया के फूल कविता में कवि ने बहुत ही मार्मिक तरीके से उसके दिल की बात कही है।
“सुबह सूरज की धूप के साथ जगाते हैं,
बैंगनी और गुलाबी रंगों के तिलिस्म
और शाम होते होते मर जाते हैं।
कवि देख रहा है कि बेहया का फूल इतना सुन्दर होने के बाद भी लोग उसे कोई उचित सम्मान नहीं देते पर कवि इसका गुलदस्ता बना के किसी अपने को भेट कर उसे सम्मान देना चाहता है। जितने भी सजीव हैं उन सबको दुख होता है। पर दुख इंसान का ही सबसे ज्यादा दिखता है अथवा लोग समझ पाते हैं। यहां कवि का एक गम्भीर चिंतन दिखाई दे रहा है पहाड़ का दुख कविता में।
पहाड़ ने इशारों में कहा-
मैं अकेला हूँ, दोस्त
आ सको तो उपर आ जाओ
पहाड़ का अकेलापन को कवि ने महसूस किया और आँखों में आँसू लिए पहाड़ की पीड़ा को समझा है।
दुनिया का हर जीव मां के बीन अधूरा है। भला ध्रुव गुप्त का कवि मन इससे अलग कैसे हो सकता है। मोह कविता में कवि मां को देह में नहीं देख रहा। उसे महसूस कर रहा है मोह में –
मां देह नहीं
मोह का अटूट सिलसिला होती है
इसलिए उसके जाने के बाद
मैं उसे मोह में ही तलासते रहता हूँ।
‘माँ और चिड़िया’ कविता में घर के रोशनदान में चिड़िया के बनाए घोसले में बैठी चिड़िया में मां को वह महसूस करता है तो वहीं ‘कहीं नहीं जाती मां’ कविता में कवि गाँव के पूराने पीपल, आँगन के तुलसी, चुल्हे चौके, गाँव के मन्दिर समेत हर उस जगह में मां को देखता है जहां शांति शीतलता व सहजता पाता है।
कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह होता है। इसका नशा एक बार चढ़ गया तो फिर उतरना मुश्किल है। उसी धर्म के नशे में आज देश मज़हबी दंगों में जल रहा है। कवि अपने कविता ‘दंगा’ में धर्म के खतरे के बीच जो सबसे बड़ी क्षति देख रहा है वह है इंसानियत की। इंसानियत के इस खतरे को पैदा करने वाले के खिलाफ खड़ा होने की बात कवि कह रहा है पर उसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है –
मैंने चीख-चीखकर कहा –
आओ, हम सब मिलकर
उनसे लड़ते हैं
जिनकी वजह से हम सब खतरे में हैं
मेरे पीछे कोई भीड़ नहीं आई।
‘कहीं कुछ अनकहा’ में ध्रुव गुप्त ने प्रकृति, प्रेम, सद्भावना, शिक्षा, धर्म, नदी, पहाड़ समेत उन तमाम चीजों को निकट से महसूस किया है जिनको आज की युवा पीढ़ी जानती नहीं अथवा जान कर भी समझती नहीं। आज टेक्नोलॉजी का युग है। सब कुछ बाजार में उपलब्ध है। ऐसे में कवि द्वारा रचित कुछ कविताएँ उस भारत का याद दिलाती हैं जो गाँव में बसता है। उसी में से एक कविता ‘जतकुटवा, है जो गांवों में जांत अथवा शिलबट्टा कूटने वालों की याद दिलाता है जो आज के मशीनी दौर में लापता हो चले हैं।
जतकुटवा अब नहीं आता
लेकिन घुटनों तक मैली धोती
पैबंद लगी गंजी
और मोटे चश्मे वाला
बचपन का वह जतकुटवा
अब भी कभी-कभी
आवाज लगा जाता है स्मृतियों में
कुल मिलाकर कहें तो ‘कहीं कुछ अनकहा’ की ज्यादातर कविताओं में कवि प्रेम, मनुष्यता और मानवीय मूल्यों को बचाने की कोशिश करता है। कुछ कविताओं में वह अपनी रचना धर्मिता से भटका हुआ भी नजर आता है। बावजूद यह पुस्तक कविता प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और सामाजिक समरसता की सोच रखने वाले पाठकों के लिए साहित्य सागर से निकाले सीप के मोती के समान है।
पुस्तक: कहीं कुछ अनकहा
लेखक: ध्रुव गुप्त
प्रकाशन: अनामिका प्रकाशन, प्रयागराज
मूल्य: 299 रुपये