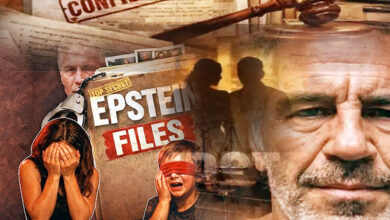संदीप ठाकुर
” गांधी गोडसे एक युद्ध “..विषय दमदार है लेकिन ट्रीटमेंट कमजोर। कहानी
जिस अंदाज में पेश की गई है वह निर्देशक की गांधी के प्रति अपरिपक्व सोच
को दर्शाता है। निर्देशक ने गांधी को बेहद हल्के अंदाज में लिया और
फुल्के अंदाज में पर्दे पर पेश कर दिया। वास्तविकता में राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी वैसे थे नहीं। जिन्हाेंने गांधी को पढ़ा नहीं और गोडसे को
जानता नहीं उसकी नजर में गोडसे हीरो बन कर उभरेगा,इस फिल्म को देखने के
बाद। फिल्म में गांधी और गोडसे के बीच संवाद की कल्पना की गयी है जिससे
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फासीवाद के चरित्र को जानता और समझता है, कभी सहमत
नहीं हो सकता। निर्माता निर्देशक ने फिल्म में कई जगह फिल्मी लिबर्टी ली
है। स्पष्ट है कि फिल्म में नाटक से अलग जो भी बदलाव किये गये हैं, उससे
लेखक की भी सहमति रही होगी। फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है,यह स्पष्ट
नहीं है। गांधी सही थे या गोडसे सही था या फिर दाेनाें अपनी अपनी जगह सही
थे ?
यह सही है कि यह फिल्म काल्पनिक कथा पर आधारित है। लेकिन यदि आप ऐतिहासिक
पात्रों और घटनाओं को आधार मानकर अपनी कल्पना प्रस्तुत करते हैं तो यह
सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि आपने उनके साथ किस हद तक और किस वजह से छूट
ली है। क्या यह महज संयोग है कि आजादी के आंदोलन और विभाजन के हिंदुस्तान
की जो व्याख्या यह फिल्म पेश करती है, वह ठीक वही क्यों है जिसे संघ
परिवार शुरू से पेश करता रहा है। गोडसे को फिल्म में आरंभ से ही एक साहसी
नायक की तरह पेश किया गया है। जबकि वह एक कायर व्यक्ति था। जब नाथूराम
गोडसे ने गांधीजी पर हमला किया था, उसके बाद वह वहां से भागने की कोशिश
करने लगा। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया तब उसने अपने को
मुसलमान बताया। ताकि गांधी की हत्या का इल्जाम मुसलमानों पर आये और देश
में दंगे भड़क उठें। लेकिन फिल्म में बताया गया है कि वह भागा नहीं बल्कि
दोनों हाथ ऊपर करके वहीं खड़ा रहा। गोडसे के विपरीत गांधीजी का
व्यक्तित्व जो फिल्म में पेश किया गया है वह एक सनकी, अपनी इच्छाएं दूसरे
पर थोपने वाला, स्त्री-विरोधी व्यक्ति का है। दरअसल यह पूरी फिल्म संघ
परिवार के राजनीतिक एजेंडे का जाने-अनजाने अनुसरण करती है। कांग्रेस और
नेहरू के प्रति जो नफरत संघ परिवार व्यक्त करता रहा है, फिल्म उस नफरत को
बढ़ाने का ही काम करती है। फिल्म पूरे विश्वास के साथ यह स्थापित करती है
कि नाथूराम गोडसे एक साहसी और सच्चा देशभक्त था।
गांधी और गोडसे दोनों ऐतिहासिक पात्र हैं। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ से संबद्ध रहा था और हिंदू महासभा का सदस्य था। 30 जनवरी
1948 को प्रार्थना सभा में जा रहे गांधी की नाथूराम ने गोली मार हत्या
कर दी थी। फिल्म में यह दिखाया गया है। लेकिन उसके बाद फिल्म काल्पनिक
हाे जाती है। हकीकत में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की मुलाकात कभी
नहीं हुई लेकिन फिल्म में यही दिखाया गया है कि नाथूराम गोडसे की गोली से
यदि गांधी बच गए होते तो क्या होता ? देश का क्या होता ? कांग्रेस का
क्या होता ? कांग्रेस के बैनर तले आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का
क्या होता ? इसके अलावा और क्या क्या हो सकता था ? इस काल्पनिक कथा पर
फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है बॉलीवुड के स्थापित निर्देशक राजकुमार
संतोषी ने। हालांकि पठान की आंधी में यह प्रयाेगात्मक फिल्म बॉक्स ऑफिस
पर तिनके की तरह उड़ गई लेकिन आज के माहौल में इतने संवेदनशील विषय पर
फिल्म बनाने व पैसे लगाने का जोखिम लेने वालों का प्रयास काबिले तारीफ
कहा जा सकता है। इस देश में सबके अपने गांधी हैं। किसी के लिए
‘राष्ट्रपिता’, किसी के लिए ‘बंटवारे का जिम्मेदार’,किसी के लिए मुस्लिम
परस्त,किसी के लिए अंग्रेजों का पिट्ठू। देखने वालों का अपना अपना नजरिया
है। लेखक असगर वजाहत और निर्देशक राजकुमार संतोषी ने भी गांधी और गोडसे
को अपने नजरिए से देखा है। उनका नजरिया क्या है यह जानने के लिए फिल्म
देखना जरूरी है।
यह फिल्म हॉलीवुड से शुरू हुए नए प्रयोग ‘व्हाट इफ’ जैसी फिल्म है। मतलब
ये कि इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में सोचना जो घटित ही नहीं हुई।
फिल्म का कॉन्सेप्ट बेजोड़ है। इस कॉन्सेप्ट का पूरा क्रेडिट जाता है
प्ले-राइट और स्क्रीन-राइटर असग़र वजाहत को, जिनके नाटक पर यह फिल्म बनी
है। असग़र वजाहत ने आज से लगभग 15 साल पहले एक नाटक लिखा था,
‘गोडसे@गांधी.कॉम’। फिल्म उसी पर आधारित है। असग़र वजाहत ने राजकुमार
संतोषी के साथ मिल कर इस फिल्म में डायलॉग भी लिखे हैं। असग़र वजाहत ने
बताया कि इस नाटक के विभिन्न भाषाओं में अनगिनत शो देश के अलग अलग
राज्यों में हाे चुके हैं। फिल्म अब बनी है। फिल्म की बेस-लाइन ये है कि
गांधी से जुड़े सारे कंटेंपरेरी तर्क वितर्क कुतर्क को फिल्म में समेटा
गया है। मसलन, गांधी का बोस के लिए क्या रवैया था ? नेहरू और पटेल के
बारे में क्या सोचते थे ? बंटवारा किसने करवाया ? अखंड भारत पर क्या
सोचते थे ? कुल मिलाकर बात ये कि पिछले कुछ सालों में वॉट्सऐप पर जो भी
आरोप लगे, गांधी ने उससे कैसे डील किया करते थे ? दूसरी ओर गोडसे को एक
कट्टर हिंदू का ही रोल दिया गया है। उसके अपने विचार थे। गांधी पर गोली
चलाने के बारे में उसकी साेच थी कि उसका यह क़दम देशहित में है। उसे लगता
था कि गांधी हठी हैं और देश को अपनी सोच पर चला रहे हैं। किसी की नहीं
सुनते। सबसे अपने विचार थोपते हैं। वह यह भी सोचता था कि केवल कांग्रेस
और गांधी ने देश को आजादी नहीं दिलाई बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद
जैसे कई ने भी गोली खाई थी। गोडसे की नजर में गांधी हिंदू विरोधी,
अंग्रेजों का एजेंट, मुसलमान प्रेमी और बंटवारे का जिम्मेदार था। गोडसे
का मानना था कि गांधी ने अहिंसा और चरखे में उलझा दिया नहीं तो 20 साल
पहले ही देश को आजादी मिल गई हाेती। फिल्म में गांधी और गोडसे, दोनों को
वैचारिक स्तर पर बदलते हुए दिखाया गया है। कैसे वो दोनों एक-दूसरे की
सोहबत में रहकर कुछ-कुछ बदले …यह बात हजम नहीं हाेती।
गांधी के रोल में दीपक आंतनी का काम जानदार है। पहले भी कई प्रोजेक्ट्स
में उन्होंने गांधी का रोल किया है। गोडसे का किरदार किया है चिन्मय
मांडलेकर ने। मराठी के जाने माने एक्टर हैं। गोडसे के रोल में वे जमे हैं
लेकिन गोडसे जैसे वे दिखते नहीं। राजकुमार संतोषी की बेटी तनीषा संतोषी
की भी इस फिल्म से सिनेमा में एंट्री हो गई है। काम उनका भी प्रभावी है।
लेकिन बतौर निर्देशक राजकुमार संतोषी की नाै साल बाद बड़े परदे पर उनकी
वापसी उतनी दमदार नहीं रही। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट ताे कम से कम यही कह
रही है। इस बात को संतोषी ने माना भी। उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज की
डेट सही नहीं रही। पठान के साथ फिल्म रिलीज नहीं करना चाहिए था। फिल्म का
अंत बहुत प्रतीकात्मक है। जेल के बाहर गांधी और गोडसे के समर्थक उनका
स्वागत करने और उन्हें लेने आते हैं लेकिन गांधी और गोडसे अपने से अपने
समर्थकों के साथ नहीं जाते। वे दोनों अपने समर्थकों के बीच से रास्ता
बनाते आगे बढ़ जाते हैं। निर्देशक ने चाहते-न चाहते गांधी और गोडसे को
समकक्ष ला खड़ा कर दिया है जिससे मेरी असहमति है। आपकी नहीं भी हो सकती
है। ठीक उसी तरह जैसे कहानीकार असगर वजाहत व निर्देशक राजकुमार संतोषी की
नहीं है।