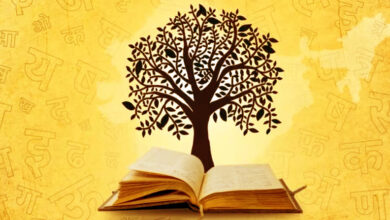डॉ. प्रियंका सौरभ
अख़बार की एक छोटी-सी खबर कई बार पूरे समाज के चेहरे से नक़ाब हटा देती है। “पढ़ाई के लिए कहने और रील बनाने से रोकने पर किशोर छोड़ रहे घर”—यह वाक्य सिर्फ़ सूचना नहीं, बल्कि हमारे समय की एक गहरी त्रासदी का बयान है। यह बताता है कि घर, जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, कई मामलों में उनके लिए असहनीय दबाव का केंद्र बनता जा रहा है। पढ़ाई, अनुशासन और भविष्य की चिंता—ये सब आवश्यक हैं, लेकिन जब ये डर, ताने, अपमान और तुलना के साथ बच्चों पर थोपे जाते हैं, तो नतीजा सीखने की प्रेरणा नहीं, बल्कि पलायन होता है। यह खबर हमें ठहरकर सोचने को मजबूर करती है कि आख़िर हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं—अंक, रैंक और प्रदर्शन या एक संतुलित, संवेदनशील और स्वस्थ मनुष्य?
आज का किशोर अभूतपूर्व बदलावों के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल दुनिया ने उसकी आंखों के सामने विकल्पों का विस्तार कर दिया है—रील्स, शॉर्ट वीडियो, ऑनलाइन दोस्ती, त्वरित प्रसिद्धि और तुरंत मिलने वाली प्रशंसा। यह सब आकर्षक है, पर इसके भीतर अस्थिरता भी है। ऐसे में परिवार की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। दुर्भाग्य से कई घरों में संवाद की जगह आदेश ने ले ली है, समझ की जगह तुलना ने, और सहानुभूति की जगह अपेक्षाओं ने। “हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं”—यह वाक्य अक्सर बच्चों के मन में भय बनकर उतरता है, क्योंकि इसके साथ उनकी बात सुनने की इच्छा नहीं जुड़ी होती।
पढ़ाई को लेकर समाज में एकांगी दृष्टि विकसित हो गई है। सफलता का पैमाना सीमित कर दिया गया है—अच्छे अंक, प्रतिष्ठित कॉलेज और तथाकथित सुरक्षित करियर। इस दौड़ में यह भूल जाता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी की रुचि विज्ञान में है, किसी की कला में; कोई खेल में खिलता है, कोई लेखन में। जब एक ही साँचे में सबको ढालने की कोशिश होती है, तो कई बच्चे टूटते हैं। वे अपनी असफलता को निजी अपराध मानने लगते हैं और धीरे-धीरे आत्मविश्वास खो देते हैं। घर छोड़ना उस टूटन का चरम बिंदु है—एक हताश प्रयास, जहाँ बच्चा भागकर शांति ढूंढना चाहता है।
किशोरावस्था वैसे ही भावनात्मक उथल-पुथल का समय है। शरीर बदलता है, मन सवालों से भरता है, पहचान गढ़ने की बेचैनी होती है। ऐसे समय में अगर घर में डांट, चिल्लाहट, तिरस्कार और निरंतर निगरानी का माहौल हो, तो बच्चा खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। कई बार माता-पिता बच्चों की चुप्पी को अनुशासन समझ लेते हैं, जबकि वह भीतर जमा होता तनाव होता है। यह तनाव कब विस्फोट बन जाए—घर छोड़ने, नशे की ओर जाने या आत्म-क्षति तक—कहना मुश्किल है।
रील्स और सोशल मीडिया को इस समस्या का एकमात्र दोषी ठहराना भी सरलीकरण होगा। यह सच है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की एकाग्रता और धैर्य को प्रभावित करता है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे स्क्रीन में शरण क्यों लेते हैं? अक्सर इसलिए क्योंकि वहाँ उन्हें सुना जाता है, सराहा जाता है, या कम-से-कम जज नहीं किया जाता। अगर घर में संवाद जीवित हो, साझा समय हो, और भरोसे का रिश्ता हो, तो डिजिटल आकर्षण संतुलन में रहता है। समस्या तकनीक नहीं, तकनीक के साथ हमारे रिश्ते की है।
माता-पिता की चिंता स्वाभाविक है। वे अपने अनुभवों से सीखकर बच्चों को कठिनाइयों से बचाना चाहते हैं। पर चिंता जब नियंत्रण में बदल जाती है, तब नुकसान होता है। बच्चों के शौक छीन लेना, दोस्तों से मिलना रोकना, हर समय तुलना करना—ये तरीके अल्पकाल में अनुशासन जैसे दिख सकते हैं, पर दीर्घकाल में विश्वास तोड़ देते हैं। बच्चा आज्ञाकारी दिखे, पर भीतर विद्रोह पनपता रहता है। पढ़ाई के प्रति प्रेम डर से नहीं, अर्थ से पैदा होता है—जब बच्चा समझता है कि वह क्यों पढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है।
स्कूल और शिक्षण संस्थानों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं। परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था बच्चों को अंक मशीन बना देती है। काउंसलिंग, लाइफ स्किल्स और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर निवेश अभी भी अपवाद है। शिक्षक अक्सर पाठ्यक्रम पूरा करने के दबाव में बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को नहीं देख पाते। स्कूल और घर अगर मिलकर एक सहायक तंत्र बनाएं—जहाँ बच्चे की रुचि, क्षमता और मानसिक स्थिति पर संवाद हो—तो बहुत-सी त्रासदियाँ रोकी जा सकती हैं।
समाज में सफलताओं का प्रदर्शन और असफलताओं का उपहास भी समस्या को बढ़ाता है। रिश्तेदारों की तुलना, पड़ोस की अपेक्षाएँ, सोशल मीडिया पर उपलब्धि का शोर—ये सब माता-पिता के दबाव को कई गुना कर देते हैं, जो आगे बच्चों पर उतरता है। हमें सामूहिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि हर रास्ता एक जैसा नहीं होता और देर से खिलने वाले फूल भी सुगंध बिखेरते हैं। जीवन रैखिक नहीं है; उसमें ठहराव, मोड़ और पुनः शुरुआत भी होती है।
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चुप्पी सबसे खतरनाक है। बच्चों की उदासी, चिड़चिड़ापन, नींद में बदलाव, पढ़ाई से अचानक दूरी—ये सब संकेत हैं, जिन्हें ‘नाटक’ या ‘जिद’ कहकर टाल देना आसान है। लेकिन समय रहते संवेदनशील हस्तक्षेप—एक शांत बातचीत, बिना टोके सुनना, जरूरत पड़े तो पेशेवर काउंसलिंग—कई जिंदगियाँ बचा सकता है। काउंसलिंग कोई कलंक नहीं, बल्कि समझदारी का कदम है।
घर के भीतर संवाद की संस्कृति बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। रोज़ का साझा समय—बिना मोबाइल, बिना आदेश—जहाँ बच्चा अपने दिन, डर और सपने कह सके। माता-पिता का यह स्वीकार करना कि उनसे भी गलती हो सकती है, बच्चों को ईमानदार बनाता है। नियम जरूरी हैं, पर नियमों के पीछे कारण बताना और बच्चों की राय सुनना उतना ही जरूरी है। अनुशासन सहमति से आए, भय से नहीं।
नीतिगत स्तर पर भी पहल आवश्यक है। स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलर, माता-पिता के लिए नियमित कार्यशालाएँ, पाठ्यक्रम में जीवन-कौशल और भावनात्मक शिक्षा का समावेश—ये कदम समय की मांग हैं। डिजिटल साक्षरता केवल तकनीक चलाना नहीं, बल्कि उसकी सीमाएँ समझना भी है। बच्चों को स्वयं-नियमन सिखाना होगा, ताकि वे स्क्रीन और पढ़ाई के बीच संतुलन बना सकें।
अंततः प्रश्न यह है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ऐसा समाज जो बच्चों को डराकर ‘सफल’ बनाता है, या ऐसा जो उन्हें समझकर सक्षम बनाता है? घर छोड़ते किशोर हमारी सामूहिक विफलता का संकेत हैं। यह केवल किसी एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का आईना है। अगर आज हम नहीं रुके, नहीं सुना, नहीं बदले—तो खबरें और भी कड़वी होंगी।
हमें याद रखना चाहिए कि बच्चे भविष्य नहीं, वर्तमान हैं। उनकी हँसी, जिज्ञासा और असहमति—सब जीवन का हिस्सा हैं। पढ़ाई महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह वातावरण जिसमें पढ़ाई होती है। जब घर दोस्ती, सम्मान और भरोसे का स्थान बनेगा, तब बच्चे भागेंगे नहीं—वे वहीं रहकर उड़ान भरेंगे। यही समय की सबसे बड़ी पुकार है, और यही हमारे हाथ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी।