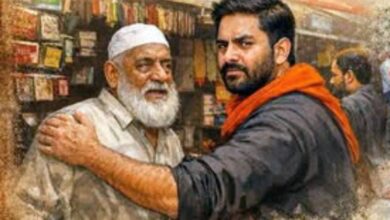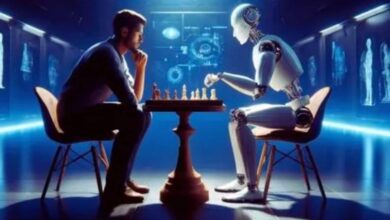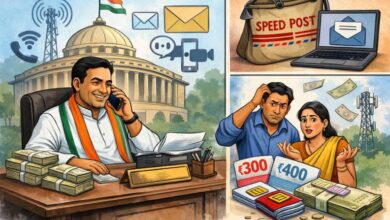नृपेन्द्र अभिषेक ‘नृप’
दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले पड़ोसी देश भारत और चीन,जब आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाते हैं, तो पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिक जाती हैं। यही दृश्य 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एस सी ओ) शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। सात वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा और 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों नेताओं का आमना-सामना, केवल औपचारिकता नहीं बल्कि विश्वास बहाली और भविष्य की साझेदारी का प्रतीक बन गया। भारत सरकार लगातार ‘पड़ोसी पहले’ और ‘साझा विकास’ की नीति पर बल देती रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने यह स्पष्ट किया कि भारत, एशिया और विश्व को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की नई सोच देना चाहता है। ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में भारत-चीन की साझेदारी न केवल द्विपक्षीय लाभ देगी, बल्कि एशिया को स्थिरता और प्रगति की राह भी दिखाएगी।
यह दौरा उस समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ़ नीतियों ने वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर दिया है। ऐसे में भारत और चीन के बीच बढ़ती निकटता एक नए आर्थिक संतुलन का संकेत देती है। यह साझेदारी एशियाई देशों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है और दुनिया को यह संदेश देती है कि संवाद, सहयोग और पारस्परिक विश्वास ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में न केवल भारत की सशक्त भूमिका को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारत वैश्विक शांति और स्थिरता का विश्वसनीय भागीदार है।
प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात महज़ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि दोनों देश सामरिक स्वायत्तता को महत्व देते हैं और उनके आपसी रिश्तों को किसी तीसरे देश की नज़र से नहीं देखा जा सकता। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत-चीन संबंध परस्पर सम्मान, विश्वास और संवेदनशीलता की बुनियाद पर खड़े होंगे। यह वक्तव्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ ने भारत के लिए आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में चीन से बढ़ती निकटता इस दबाव को संतुलित करने का व्यावहारिक उपाय बन सकती है।
भारतीय हाथी और चीनी ड्रैगन का साथ आना एक प्रकार से एशिया की नई शक्ति संतुलन की कहानी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं स्वीकार किया कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार हैं। उनका यह कथन कि “दोनों देश एक-दूसरे के विकास के अवसर हैं, खतरा नहीं” रिश्तों में नई मिठास घोलता है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने यह भी माना कि मतभेद झगड़े में तब्दील नहीं होने चाहिए। यह बयान दोनों देशों की परिपक्वता और जिम्मेदारी का परिचायक है।
सीमा विवाद और आर्थिक साझेदारी
भारत-चीन रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा सीमा विवाद रही है। 1962 का युद्ध और 2020 की गलवान घाटी की झड़पें इसका प्रमाण हैं। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों ने कई स्तरों पर बातचीत कर स्थिति को स्थिर करने की कोशिश की है। विशेष प्रतिनिधियों की बैठकों ने सीमा पर डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया को गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में यह भी कहा कि पिछले साल फौज वापसी प्रक्रिया के बाद सीमा पर स्थिरता आई है, जो दोनों देशों के लिए शुभ संकेत है। चीन भी यह समझ चुका है कि लंबे समय तक तनाव बनाए रखना न तो उसके लिए हितकारी है और न ही भारत के लिए।
आज भारत और चीन दुनिया की कुल आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा समेटे हुए हैं और वैश्विक जीडीपी में 20 प्रतिशत योगदान करते हैं। ऐसे में दोनों देशों का आर्थिक सहयोग पूरे विश्व अर्थतंत्र पर असर डालता है। वर्तमान में भारत-चीन व्यापार घाटा 99 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन तियानजिन बैठक में यह संकेत मिले कि चीन भारत के लिए अपने बाजार को और अधिक खोलने पर विचार कर सकता है। बीजिंग द्वारा दुर्लभ धातुओं, उर्वरकों और मशीनरी की आपूर्ति को लेकर चर्चा इसी दिशा में सकारात्मक कदम है।
शंघाई सहयोग संगठन और भारत की भूमिका
एस सी ओ मंच पर भारत और चीन का साथ आना बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूती देता है। इस संगठन के देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है और यह वैश्विक तेल-भंडार का 20% हिस्सा नियंत्रित करते हैं। ऐसे में इस मंच पर भारत-चीन सहयोग अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला ठोस कदम माना जा रहा है। एस सी ओ के माध्यम से दोनों देश न केवल आर्थिक बल्कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर भी साझेदारी बढ़ा सकते हैं।
भारत आज न तो पूरी तरह चीन के खेमे में जा सकता है और न ही अमेरिका के। यही भारत की ताकत है कि वह अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन साधता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को “ग्लोबल स्विंग पावर” बनना चाहिए, यानी ऐसी शक्ति जिस पर चीन और अमेरिका दोनों अपने हित साधने के लिए निर्भर हों। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है, जहां भारत अपनी आर्थिक क्षमता और जनशक्ति का इस्तेमाल कर वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
भारत और चीन के संबंधों का अतीत उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। आज़ादी के शुरुआती दिनों में “हिन्दी-चीनी भाई-भाई” का नारा गूंजा था, पर 1962 के युद्ध ने भरोसे की नींव हिला दी। उसके बाद सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और पाकिस्तान को चीन का समर्थन भारत-चीन रिश्तों को बार-बार उलझाता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की लगातार मुलाकातें, चाहे वह कजान (2024) हो या तियानजिन (2025), यह बताती हैं कि दोनों देशों ने मतभेदों के बावजूद संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं किया।
चीन-पाकिस्तान समीकरण और भारत की चिंताएं
भारत-चीन संबंधों में सबसे बड़ी जटिलता पाकिस्तान को लेकर रही है। भारत की चिंता यह रही है कि चीन लगातार पाकिस्तान को रणनीतिक सहयोग देता आया है, चाहे वह रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हो या बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश। इस सहयोग से भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक हित प्रभावित होते रहे हैं। हालांकि, हाल की घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि चीन भी अब भारत की संवेदनशीलताओं को समझने लगा है। शंघाई सहयोग संगठन (एस सी ओ) की एक महत्वपूर्ण बैठक में चीन ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर प्रत्यक्ष समर्थन देने से परहेज़ किया। यह बदलाव भारत की सक्रिय कूटनीति की सफलता माना जा सकता है, जिसने चीन को यह संदेश देने में सफलता पाई कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता।
भारत की कोशिश हमेशा से यह रही है कि चीन आतंकवाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों पर भारत की चिंता और दृष्टिकोण को गंभीरता से स्वीकार करे। अगर चीन इस दिशा में और कदम आगे बढ़ाता है, तो न केवल भारत-चीन रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भी मजबूती मिलेगी। इस तरह, पाकिस्तान के संदर्भ में चीन का बदला हुआ रुख भविष्य के सहयोग की नई संभावनाएँ खोल सकता है।
भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताएँ हैं। दोनों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ऐतिहासिक रिश्ते हजारों वर्षों पुराने हैं। बौद्ध धर्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल के वर्षों में कैलाश-मानसरोवर यात्रा का पुनः प्रारंभ और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना इस रिश्ते में नई गर्मजोशी लाता है। यह समझना होगा कि केवल रणनीतिक और आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी दोनों देशों को जोड़ते हैं।
विश्वास की खाई पाटने की दिशा में एक कदम
भारत और चीन के रिश्तों की जटिलताओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोनों देशों को अभी लंबा सफ़र तय करना है। दशकों से चली आ रही अविश्वास की खाई को पाटना आसान नहीं है, और इसके लिए सबसे पहली शर्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान है। जब तक सीमा पर तनाव बना रहेगा, तब तक आपसी संबंधों में पूरी तरह विश्वास कायम करना कठिन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में तियानजिन में इस बात पर ज़ोर दिया कि सीमा की स्थिरता ही सहयोग का आधार बन सकती है। चीन भी यह समझने लगा है कि लंबे समय तक तनाव बनाए रखना उसके आर्थिक हितों और वैश्विक छवि के लिए बाधा ही बनेगा।
भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती व्यापार असंतुलन की है। वर्तमान में भारत चीन से कहीं अधिक आयात करता है, जबकि उसका निर्यात बहुत सीमित है। यह असंतुलन भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है। ऐसे में भारत की प्राथमिकता है कि व्यापार संबंधों को अधिक संतुलित और परस्पर लाभकारी बनाया जाए। चीन के विशाल बाजार तक भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की पहुँच बढ़ाना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है। फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात ने यह आशा जगाई है कि दोनों देश व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने को तैयार हैं। यह मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संकेत है कि सहयोग की दिशा में ठोस कदम संभव हैं। यदि यह रुझान कायम रहता है, तो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता और विकास की नई संभावनाएँ खुल सकती हैं।
आज की दुनिया में स्थायी दुश्मन और स्थायी मित्र जैसी कोई अवधारणा नहीं बची है। बदलते वैश्विक समीकरणों ने भारत और चीन दोनों को यह अहसास कराया है कि परस्पर सहयोग ही स्थायी शांति और विकास का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तियानजिन मुलाकात इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश इतिहास की कड़वाहट से आगे बढ़कर भविष्य की ओर देखना चाहते हैं। भारत और चीन का साथ केवल एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक संदेश है। यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता देगा बल्कि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज़ को भी मजबूत करेगा। हाथी और ड्रैगन का यह नया नृत्य आने वाले समय में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने वाला साबित हो सकता है।