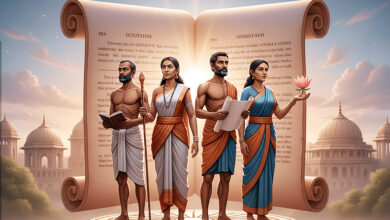डॉ. दीपक आचार्य
निरन्तर बढ़ती जा रही ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय खतरों के चलते अधिकाधिक पौधारोपण के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रयासों की आवश्यकता आज हर कहीं महसूस हो रही है।
सरकार के साथ ही समाजों, संस्थाओं, विभागों, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों एवं पर्यावरण प्रेमियों द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। ख़ासकर मरुभूमि में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण आज की पहली जरूरत है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में कई प्रयास जारी हैं यद्यपि मरुप्रदेश में पानी की कमी, रेतीली और पथरीली भूमि जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पौधे लगाने और उन्हें पल्लवित करने का काम मुश्किलों भरा है।
इसे आसान कर दिखाया है सरकार की एक अभिनव पहल ने, जिसे ‘मटका थिम्बक’ पद्धति कहा जाता है। जोधपुर जिले में इसका प्रयोग पौधारोपण आशातीत सफलता दर्शा रहा है।
अनुकरणीय है तिलवासनी का चारागाह विकास कार्य
जोधपुर जिले की पीपाड़शहर पंचायत समिति अन्तर्गत तिलवासनी ग्राम पंचायत का चारागाह इसी का ज्वलन्त उदाहरण दे रहा है। तिलवासनी में खसरा नम्बर 212 में 9 लाख 98 हजार रुपए धनराशि से 2019-20 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत चारागाह विकास कार्य स्वीकृत किया गया तथा 6 लाख 89 हजार की धनराशि व्यय कर पूर्ण किया गया।
इसमें लगाए गए कुल 300 पौधों में से 250 पौधे जीवित हैं और इनका सुरक्षित पल्लवन व विकास हो रहा है। और इसके पीछे मटका थिम्बक पद्धति का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत तिलवासनी के सरपंच श्री अनिल बिश्नोई ने चारागाह में पौधारोपण के लिए मटका पद्धति के इस प्रयोग की अनुकरणीय पहल की है, जिसके उत्साहजनक एवं आशातीत परिणाम सामने आए हैं।
मरुभूमि के लिए कारगर है प्रयोग
बूंद-बूंद सहेजते हुए पौधे लगाने और हरियाली बढ़ाने की इस अनूठी पहल की शुरुआत मरुभूमि पर्यावरण विकास में शुभ संकेत है। इस पद्धति में जल संरक्षण और पौधारोपण के मध्य बेहतर सामंजस्य का दिग्दर्शन हो रहा है।
मटका थिम्बक पद्धति के बारे में मान्यता है कि यह 4 हजार साल पुरानी सिंचाई पद्धति है जिसका प्रयोग ईरान, दक्षिण अमरीका आदि में किया जा रहा है। इसके बाद भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, जर्मनी जैसे देशों ने भी इसे अपनाया। मटका सिंचाई पद्धति का जिक्र कृषि विज्ञान पर लिखी गई पहली किताब फेन-शेंग ची-शू में किया गया है। किताब के मुताबिक, चीन में इस पद्धति का प्रयोग 2 हजार साल से भी ज्यादा पुराना है।
पौधों का सुरक्षित पल्लवन हुआ आसान
मरुप्रदेश में चारागाहों में पौधारोपण के लिए अब इस पद्धति का प्रयोग अमल में लाया जा रहा है और इसे अपनाया जाकर पौधारोपण होने लगा है।
आम तौर पर पौधारोपण के बाद पौधों के सुरक्षित पल्लवन और विकास के लिए नियमित रूप से सिंचाई जरूरी होती है लेकिन कभी-कभार रोजमर्रा की जिन्दगी में व्यस्तता के कारण से अथवा भूलवश सिंचाई करना भूल जाने की स्थिति में पौधों के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
इसी प्रकार सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी अथवा सिंचाई प्रबन्धन की कमी के कारण भी समस्या पैदा हो जाती है और ऐसे में पौधों की सुरक्षा और विकास के लिए बहुत अधिक परिश्रम किए जाने की स्थिति आ जाती है। इन सभी परिस्थितियों में मटका थिम्बक पद्धति बेहद कारगर सिद्ध होती है।
यह है मटका सिंचाई पद्धति
एक मटका लें और उसे पौधे के पास जमीन में गड्ढा खोद रख दें। मटका इस तरह रखा जाए कि उसका मुँह जमीन के बाहर रहे। मटके को ऊपर तक पानी से भर दें। मटके के छिद्रों से पानी रिस-रिस कर पेड़ की जड़ों तक पहुंचेगा और उसको सींचेगा। पौधे के आस-पास घास-फूस, पत्तियां डाल दें ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रह सके। मटके को कवर करके रखें। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बरसों से इस पद्धति का प्रयोग हरियाली विस्तार का माध्यम बना हुआ है।
कई ख़ासियतों भरी है मटका पद्धति
मटका सिंचाई पद्धति से 70 फीसदी तक पानी बच सकता है। जोधपुर, बाड़ेमर जैसे रेतीले इलाके में यह पद्धति बेहद कारगर साबित हो सकती है। लोग पौधों को न केवल लगा रहे बल्कि उनको सहेज भी रहे हैं। पौधों की परिजनों की तरह देखभाल की जा रही है। उचित देखभाल से पौधों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। हरियाली बढने से मन को भी सुकून मिलने लगा है।
यह पद्धति मिट्टी, पौधों की सेहत और आय तीनों के लिए फायदेमंद है। मटका सिंचाई पद्धति से पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। सिंचाई पद्धति से पूरे साल फसल उत्पादन संभव है। मटका भरने की जरूरत 20-24 घंटे में पड़ती है। इस पद्धति में पानी के साथ समय की बचत होती है। कम संसाधन और आसान तकनीक अपनाने से ही पौधे का विकास भी तेजी से होता दिखता है।
सबसे आसान है यह तकनीक
इस पद्यति के द्वारा फलों और सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। इसमें सबसे कम मात्रा में पानी की खपत होती है यानी पानी की ज्यादा-से-ज्यादा बचत की जा सकती है। यह एक ऐसी सरल, सहज और बिना पैसों की तकनीक है, जिससे कम पानी में भी पौधा जीवित रह सकता है और पानी का भी अपव्यय नहीं होता। मरुस्थल में अब इस तकनीक के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है।