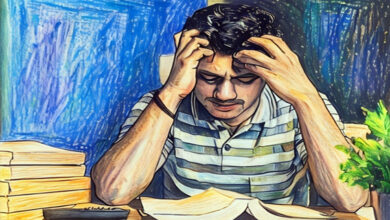संजय सक्सेना
बरेली के महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक डॉ. रजनीश गंगवार द्वारा पढ़ी गई कविता “तुम कांवड़ लेने मत जाना” पर मचा बवाल सिर्फ एक कविता पर विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत में धार्मिक आस्था, शिक्षा, तर्क और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच खिंची उस लकीर का उदाहरण है जो आज की तारीख में लगातार गहरी होती जा रही है। यह मामला दिखाता है कि आज के समय में शिक्षक, विद्यार्थी, समाज और राजनीति के बीच की संवेदनशील रेखाएं कितनी धुंधली होती जा रही हैं। कविता का मूल भाव यदि देखा जाए, तो छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना था। लेकिन जिस रूप में यह बात कही गई, उसमें धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग इस तरह किया गया कि मामला श्रद्धा और तिरस्कार के बीच फंस गया। कविता की पंक्तियां थीं, “कांवड़ ढोकर कोई डीएम, एसपी नहीं बना है। भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा मद से कोई उद्धार नहीं हुआ है। तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना।” शब्दों की गहराई को देखें तो यह सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि कटाक्ष था। ‘कांवड़’, ‘गांजा’, ‘धतूरा’, ‘सुल्फा’ जैसे शब्दों का संयोजन उस धार्मिक परंपरा पर प्रश्नचिह्न लगाता है जो करोड़ों लोगों के लिए एक श्रद्धा है। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। इसमें सामूहिकता, अनुशासन, सेवा और संकल्प का भाव होता है। ऐसे में जब एक शिक्षक इसे इस तरह चित्रित करता है कि जैसे यह सिर्फ नशे और फालतूपन का प्रतीक है, तो समाज के एक बड़े हिस्से में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है।
कविता के पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि शिक्षक ने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए यह उदाहरण दिया। लेकिन क्या प्रेरणा देने के लिए धार्मिक परंपराओं को नीचा दिखाना जरूरी हो जाता है? क्या कोई शिक्षक यह नहीं कह सकता था कि ‘शिक्षा ही सर्वोत्तम साधना है’ या ‘ज्ञान का मार्ग ही सफलता का मार्ग है’ बिना किसी धर्म, परंपरा या भावना पर कटाक्ष किए? जब बात शिक्षा की होती है, तो तटस्थता सबसे जरूरी तत्व बन जाती है। एक शिक्षक का हर शब्द विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव डालता है, ऐसे में उसकी बातों में संतुलन और संवेदनशीलता दोनों होनी चाहिए।
इस कविता की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इसका संदर्भ भले ही शिक्षा था, लेकिन भाषा और प्रतीकों की वजह से यह सीधे धर्म से टकरा गई। और जब मामला धर्म बनाम शिक्षा में तब्दील होता है, तो वह केवल कक्षा तक सीमित नहीं रह जाता। फिर वह समाज की सड़कों पर उतर आता है। यही इस मामले में हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, एफआईआर दर्ज हुई, शिक्षक को सस्पेंड किया गया और मामला राजनीतिक रंग में रंग गया। यहां यह सवाल उठता है कि क्या हमारे शिक्षक शिक्षा के नाम पर वैचारिक प्रचार कर रहे हैं? क्या यह कविता केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक थी या किसी गहरे वैचारिक आग्रह की परिणति थी? डॉ. गंगवार का अतीत अगर देखा जाए तो वे एक समय एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी कविता उस विचारधारा से मेल नहीं खाती। बल्कि उन्होंने जिस प्रकार की भाषा और प्रतीक का इस्तेमाल किया, वह उन्हीं लोगों की धार्मिक परंपराओं पर कटाक्ष करती है जिनके बीच वे पहले खड़े रहे थे। इसलिए एबीवीपी ने भी तुरंत उन्हें निलंबित कर दिया। यह विरोधाभास इस बात का संकेत है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब केवल ज्ञान नहीं, विचारधारा भी प्रवेश कर चुकी है।
भारत जैसे देश में, जहां धर्म केवल आस्था का नहीं, बल्कि जीवन पद्धति का हिस्सा है, वहां किसी धार्मिक परंपरा को इस प्रकार नकारात्मक रूप में दिखाना केवल विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन को गहरा करना है। यह विभाजन दो ध्रुवों में बंटता जा रहा है एक ओर वे लोग हैं जो तर्क, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरी ओर वे हैं जो परंपरा, आस्था और धार्मिकता को अपनी पहचान का मूल मानते हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि ये दोनों विचारधाराएं एक-दूसरे की विरोधी हों? क्या हम ऐसा समाज नहीं बना सकते, जहां एक बच्चा शिवभक्त भी हो और वैज्ञानिक सोच वाला भी? क्या वह कांवड़ भी उठा सकता है और आईएएस भी बन सकता है? भारत का इतिहास तो यही कहता है कि यहां धर्म और ज्ञान साथ चलते हैं।
इस पूरे विवाद में एक और पहलू जो ध्यान देने लायक है, वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। डॉ. गंगवार ने माफीनामा जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म का अपमान नहीं था। लेकिन भारत का संविधान भी यही कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती। अनुच्छेद 19(2) के तहत, यह स्वतंत्रता कुछ सीमाओं के भीतर ही स्वीकार्य है, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और दूसरों की भावनाएं शामिल हैं। एक शिक्षक को यह समझना चाहिए कि वह कक्षा में जो कहता है, वह केवल विचार नहीं, बल्कि मूल्य बनकर विद्यार्थियों के मन में बस जाता है। इसीलिए शिक्षकों के शब्दों में विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए। वे अगर कुछ कहना भी चाहते हैं, तो उसमें कटाक्ष नहीं, सहमति और संतुलन होना चाहिए।
राजनीतिक प्रतिक्रिया ने भी इस मामले को और जटिल बना दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉ. गंगवार के समर्थन में बयान दिया और कहा कि एक शिक्षक बच्चों को ज्ञान की बात कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर करना असहिष्णुता है। यह बात एक सीमित नजरिए को दर्शाती है। सवाल यह है कि अगर यही कविता किसी अन्य धर्म की धार्मिक यात्रा पर होती, तो क्या यही समर्थन होता? क्या यही लोग तब भी खड़े होते? यह दोहरा मापदंड भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है।
यह विवाद एक आईना है, जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक हस्तक्षेप तीनों को साफ देखा जा सकता है। शिक्षक अब केवल पढ़ाने वाले नहीं रह गए, वे अब विचारधारा का माध्यम भी बनते जा रहे हैं। यह स्थिति खतरनाक है। अगर कक्षा में ज्ञान के स्थान पर तिरस्कार परोसा जाने लगे, तो भविष्य का समाज असंतुलित और बंटा हुआ होगा। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि हमें अपने शिक्षकों को केवल विषय विशेषज्ञ नहीं, बल्कि संवेदनशील विचारक बनाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विद्यार्थियों को प्रेरित करें बिना किसी विश्वास या परंपरा को नीचा दिखाए। शिक्षा का काम बच्चों को सोचने की क्षमता देना है, न कि उन्हें किसी खास दिशा में मोड़ना। अगर शिक्षक अपनी बात को कहने के लिए किसी समुदाय की आस्था पर हमला करेगा, तो वह शिक्षक नहीं, प्रचारक कहलाएगा।
अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि “तुम कांवड़ लेने मत जाना” जैसी कविताएं अगर छात्रों को पढ़ाई की ओर ले जाती हैं, तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें न व्यंग्य हो, न तिरस्कार। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षक अगर इस संतुलन को नहीं साध सके, तो फिर कौन साधेगा? इस मामले में केवल शिक्षक नहीं, पूरा समाज कठघरे में है। हमें यह तय करना होगा कि शिक्षा को कैसे एक ऐसी भूमि बनाई जाए जहां सभी विचार, सभी विश्वास, और सभी रास्ते साथ चल सकें। यही भारतीयता है, यही भारत की आत्मा है।