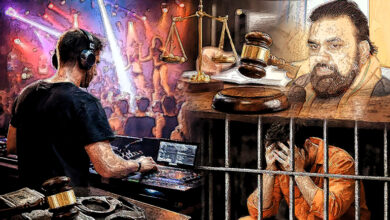(एक से अधिक पेंशन, यात्रा भत्ते की सर्वसम्मति और 60 साल सेवा के बाद भी पेंशन से वंचित कर्मचारी—लोकतंत्र की उलटी प्राथमिकताओं की कहानी)
सवाल राशि का नहीं, नियत का है। सवाल यह है कि जब एक आम कर्मचारी 30–35 साल सेवा देने के बाद भी पेंशन के लिए दर-दर भटकता है, जब लाखों कर्मचारी नई पेंशन योजना के जाल में फँसकर बुढ़ापे की सुरक्षा से वंचित हैं, तब सत्ता से जुड़े लोगों को एक से अधिक पेंशन किस नैतिक अधिकार से मिलती है?
यह कैसी व्यवस्था है जहाँ विधायक बनने के पाँच साल बाद भी पेंशन का अधिकार जन्म ले लेता है, लेकिन शिक्षक, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, फील्ड वर्कर—जो 60 साल तक सेवा देता है—वह पेंशन का पात्र भी नहीं बन पाता? क्या लोकतंत्र में श्रम का मूल्य सत्ता की दूरी से तय होता है?
डॉ सत्यवान सौरभ
लोकतंत्र की किताबों में लिखा है कि सत्ता जनता की सेवक होती है। व्यवहार में यह वाक्य अब एक पुराना मुहावरा बन चुका है—इतना पुराना कि सत्ता खुद भी इसे गंभीरता से नहीं लेती। आज का लोकतंत्र सेवा नहीं, सुविधा का तंत्र बन चुका है; और इस तंत्र की सबसे सुंदर, सबसे सुविधाजनक, सबसे सुरक्षित जगह है—सर्वसम्मति।
जैसे ही बात अपने हितों की आती है, हमारे जनप्रतिनिधि वैचारिक मतभेद भूल जाते हैं। न पक्ष रहता है, न विपक्ष। न सत्ता होती है, न प्रतिपक्ष। सब एक साथ हो जाते हैं—जैसे कोई पारिवारिक मामला हो, जैसे कोई निजी उत्सव हो। पूर्व विधायकों के लिए ₹10,000 यात्रा भत्ता का सर्वसम्मति से पारित होना कोई साधारण निर्णय नहीं है, यह उस मानसिकता का उद्घाटन है जिसमें सत्ता खुद को जनता से ऊपर और अलग मानने लगती है।
यह वही सदन है जहाँ किसानों की आत्महत्याओं पर बहस “असंवेदनशील” हो जाती है, मज़दूरों की मौतें “आँकड़ों” में बदल जाती हैं, बेरोज़गारी “वैश्विक चुनौती” बन जाती है और महँगाई “अस्थायी स्थिति” कहकर टाल दी जाती है। लेकिन जैसे ही बात विधायकों, पूर्व विधायकों, मंत्रियों या सत्ता से जुड़े वर्ग की आती है—लोकतंत्र चौकन्ना हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तत्पर हो जाता है।
₹10,000 कोई बड़ी राशि नहीं है—यह तर्क अक्सर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। यह बड़ी राशि नहीं है। लेकिन सवाल राशि का नहीं, नियत का है। सवाल यह है कि जब एक आम कर्मचारी 30–35 साल सेवा देने के बाद भी पेंशन के लिए दर-दर भटकता है, जब लाखों कर्मचारी नई पेंशन योजना के जाल में फँसकर बुढ़ापे की सुरक्षा से वंचित हैं, तब सत्ता से जुड़े लोगों को एक से अधिक पेंशन किस नैतिक अधिकार से मिलती है?
यह कैसी व्यवस्था है जहाँ विधायक बनने के पाँच साल बाद भी पेंशन का अधिकार जन्म ले लेता है, लेकिन शिक्षक, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, फील्ड वर्कर—जो 60 साल तक सेवा देता है—वह पेंशन का पात्र भी नहीं बन पाता? क्या लोकतंत्र में श्रम का मूल्य सत्ता की दूरी से तय होता है?
विडंबना यह है कि जिन पूर्व विधायकों को आज यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, वे पहले से ही कई-कई पेंशन ले रहे हैं—कभी विधायक की, कभी सांसद की, कभी मंत्री की, कभी समिति की। सत्ता में बिताए गए कुछ वर्षों ने उन्हें आजीवन सुरक्षा दे दी, जबकि वही सत्ता व्यवस्था को चलाने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में भी असुरक्षित छोड़ देती है।
जनता से बार-बार कहा जाता है कि “सरकार के पास पैसा नहीं है।” लेकिन यह वाक्य केवल जनता के लिए आरक्षित है। कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है, छात्रों के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। लेकिन नेताओं की सुविधाओं के लिए पैसा हमेशा उपलब्ध रहता है—बिना बहस, बिना विरोध, बिना शर्म।
सवाल यह भी है कि विरोध आखिर जाता कहाँ है? जिन सदनों में पानी की बोतल पर हंगामा हो जाता है, जहाँ शब्दों पर माइक टूट जाते हैं, जहाँ तख्तियाँ और पोस्टर लोकतंत्र का पर्याय बन जाते हैं—वहीं इस फैसले पर पूर्ण शांति कैसे छा जाती है? क्या सत्ता और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सुविधाओं के मुद्दे राजनीति से ऊपर हैं?
यह वह अघोषित समझौता है, जिसके बारे में जनता को कभी बताया नहीं जाता। चुनाव के समय दल एक-दूसरे के खिलाफ ज़हर उगलते हैं, लेकिन सत्ता के लाभों के समय सभी ज़हर मीठे शरबत में बदल जाते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, सुविधातंत्र है।
सबसे भयावह स्थिति तब बनती है जब इस सबको “कानूनी” कहकर जायज़ ठहराया जाता है। हाँ, यह सब कानूनी है। लेकिन क्या हर कानूनी चीज़ नैतिक भी होती है? इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े अन्याय कानून की छाया में ही हुए हैं। अगर कानून जनता की कीमत पर सत्ता की सुविधा सुनिश्चित करे, तो उस कानून पर सवाल उठाना नागरिक कर्तव्य बन जाता है।
आज देश का कर्मचारी वर्ग सबसे ठगा हुआ वर्ग है। नई पेंशन योजना के नाम पर उसकी सामाजिक सुरक्षा छीन ली गई। 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद भी उसे यह भरोसा नहीं कि बुढ़ापे में दवा, इलाज और सम्मानजनक जीवन मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर, सत्ता से जुड़े लोग पेंशन को अधिकार नहीं, विशेषाधिकार बना चुके हैं—और उस विशेषाधिकार पर किसी तरह का आत्मसंयम दिखाना उन्हें ज़रूरी नहीं लगता।
यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता नहीं, नैतिक दिवालियापन की निशानी है। जब सत्ता खुद के लिए संवेदनशील और जनता के लिए कठोर हो जाए, तब लोकतंत्र केवल एक शब्द रह जाता है—एक खोखला शब्द।
आज जनता को बार-बार यह एहसास कराया जा रहा है कि सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है, असहमति अराजकता है और विरोध अनुशासनहीनता। लेकिन सत्ता की सुविधाओं पर चुप्पी ही सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि यह चुप्पी उस असमानता को मजबूत करती है, जो समाज को भीतर से खोखला कर देती है।
पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ते पर सर्वसम्मति कोई उपलब्धि नहीं है। यह उस सोच का प्रमाण है जिसमें सत्ता खुद को विशेष वर्ग मान चुकी है। यह निर्णय एक चेतावनी है कि अगर लोकतंत्र केवल सत्ता के लिए एकमत होता रहा, तो जनता की असहमति एक दिन सर्वसम्मति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होकर सामने आएगी।
इतिहास गवाह है—जब शासक वर्ग अपनी सुविधाओं में डूब जाता है और जनता के दुखों से कट जाता है, तब सत्ता स्थायी नहीं रहती। सिंहासन हमेशा मजबूत नहीं होता, लेकिन जनता की स्मृति बहुत लंबी होती है।
हाँ, आप बधाई के पात्र हैं—इसलिए नहीं कि आपने कोई महान जनहितकारी निर्णय लिया, बल्कि इसलिए कि आपने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारे लोकतंत्र में अपने लिए सर्वसम्मति है, और जनता के लिए प्रतीक्षा।
और यह प्रतीक्षा जब बहुत लंबी हो जाती है, तो वह एक दिन सवाल बनती है— और सवाल, इतिहास की सबसे खतरनाक चीज़ होते हैं।