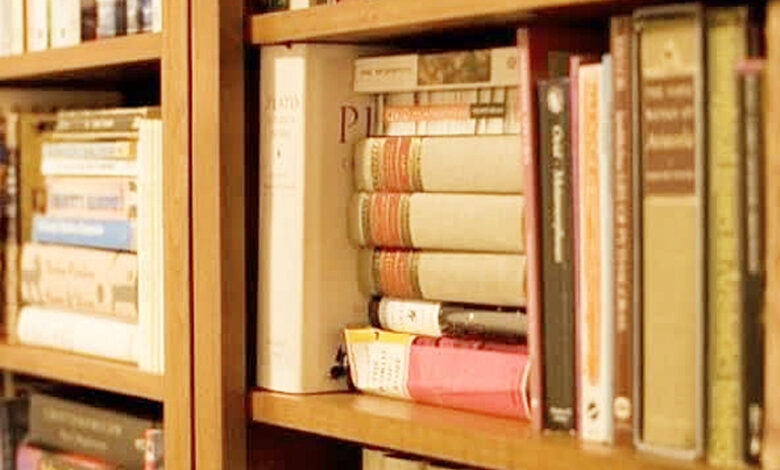
विजय गर्ग
1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, भारत ने पुस्तकालय सुधारों की एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की है, जो औपनिवेशिक और रियासत के पुस्तकालयों के बिखरे हुए संग्रह को अधिक संरचित में बदल रही है, हालांकि अभी भी विकसित हो रही है, राष्ट्रीय प्रणाली। स्वतंत्रता के बाद से 78 वर्षों को प्रमुख कानून, प्रभावशाली संस्थानों की स्थापना और एक लोकतांत्रिक और साक्षर समाज में पुस्तकालयों की भूमिका की बढ़ती मान्यता द्वारा चिह्नित किया गया है। यहां स्वतंत्रता के बाद से भारत में पुस्तकालय सुधारों की यात्रा का अवलोकन किया गया है: प्रारंभिक स्वतंत्रता के बाद का युग (1947-1960)
राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना: स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख और तत्काल कदम कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसने एक औपनिवेशिक संस्थान से राष्ट्रीय गौरव और ज्ञान के प्रतीक में बदलाव का संकेत दिया।
पुस्तकालय विधान: पुस्तकालय सुधार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक राज्य-स्तरीय पुस्तकालय कानून के लिए धक्का रहा है। इनमें से पहला कार्य, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, 1948 में पारित किया गया था, मोटे तौर पर डॉ के प्रयासों के कारण। एसआर रंगनाथन, जिसे अक्सर “भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक” कहा जाता है। इस अधिनियम, और बाद के अन्य राज्यों में, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालियों की स्थापना, रखरखाव और वित्तपोषण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया।
द डिलीवरी ऑफ बुक्स (पब्लिक लाइब्रेरी) एक्ट, 1954: इस ऐतिहासिक कानून में कहा गया है कि भारत में प्रकाशकों को कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, चेन्नई में कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित होने वाली हर किताब की एक प्रति जमा करनी होगी। बॉम्बे, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इस अधिनियम ने देश के साहित्यिक उत्पादन के संरक्षण को सुनिश्चित किया।
** दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (1951): यूनेस्को की मदद से स्थापित, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक आधुनिक, मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के लिए एक मॉडल थी। इसने मोबाइल पुस्तकालयों जैसी सेवाओं का बीड़ा उठाया और दूसरों का अनुसरण करने का एक खाका बन गया।
पंचवर्षीय योजनाएं: भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं ने पुस्तकालयों के महत्व को मान्यता दी। पहली योजना (1951-1956) का उद्देश्य राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करना था। दूसरी योजना (1956-1961) ने सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया।
मध्य अवधि (1970s-1990s
राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन (आरआरआरएलएफ): भारतीय पुस्तकालय आंदोलन में एक वाटरशेड पल 1972 में आरआरआरएलएफ की स्थापना थी। संस्कृति मंत्रालय के तहत यह नींव सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का समर्थन और प्रचार करने के लिए नोडल एजेंसी बन गई। यह पुस्तकालयों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, नए पुस्तकालयों के गठन को प्रोत्साहित करता है, और पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करता है।
अधिक राज्य-स्तरीय विधान: पुस्तकालय कानून के लिए धक्का जारी रहा। आंध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (1965), महाराष्ट्र (1967), और पश्चिम बंगाल (1979) जैसे राज्यों ने अपने स्वयं के पुस्तकालय अधिनियम बनाए, जिससे देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों का अधिक व्यापक नेटवर्क बन गया।
पुस्तकालय और सूचना प्रणाली (NAPLIS) पर राष्ट्रीय नीति: 1980 के दशक में, पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। परिणामी दस्तावेज, जबकि कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिनियम नहीं है, एक समन्वित राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के लिए एक दृष्टि प्रदान की और धन, मानव संसाधन, और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे मुद्दों को संबोधित किया । आधुनिक युग और चुनौतियां (2000-वर्तमान)
डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण: इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के आगमन के साथ, पुस्तकालय सुधारों का ध्यान स्थानांतरित हो गया है। पुस्तकालय संग्रह को डिजिटल बनाने, डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने और संसाधनों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए पहल चल रही है। आरआरआरएलएफ इसमें एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, जो डिजिटल पुस्तकालयों और रिपॉजिटरी के निर्माण का समर्थन करता है।
चुनौतियां और अंतराल: महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारतीय पुस्तकालय प्रणाली अभी भी चुनौतियों का सामना कर रही है। एक प्रमुख मुद्दा कई राज्यों में पुस्तकालय कानून की कमी है, जो असंगत धन और एक संरचित पुस्तकालय नेटवर्क की कमी की ओर जाता है। कई स्थानों पर, मौजूदा पुस्तकालय अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और पुराने संग्रह से पीड़ित हैं।
पुस्तकालयों की बदलती भूमिका: आधुनिक पुस्तकालय अब केवल पुस्तकों का भंडार नहीं है। यह एक सामुदायिक केंद्र, सूचना, शिक्षा और सामाजिक संपर्क के लिए एक केंद्र में विकसित हो रहा है। इस नई भूमिका के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है, जो इंटरनेट एक्सेस, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य समुदाय-आधारित सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अंत में, भारत में 78 साल के पुस्तकालय सुधार निर्माण और विकसित होने की एक सतत प्रक्रिया रही है। राष्ट्रीय पहचान और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने पर प्रारंभिक ध्यान देने से, यात्रा अब प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और पुस्तकालयों को ज्ञान और सामुदायिक जुड़ाव के गतिशील केंद्रों में बदलने की ओर बढ़ गई है।







