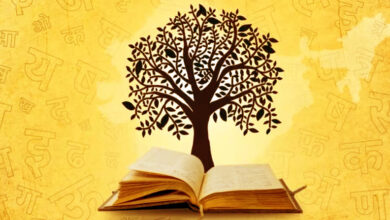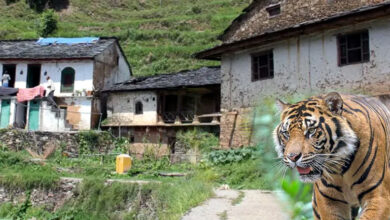बिशन पपोला
बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित घटनाओं और अनपेक्षित गठबंधनों के लिए जानी जाती रही है। जहां का राजनीतिक परिदृश्य न सिर्फ जातीय समीकरणों पर टिका होता है, बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और क्षणिक अवसरवाद भी उसमें बराबरी का स्थान रखते हैं। इसी पृष्ठभूमि में पप्पू यादव और भाजपा के बीच 2015 में जो समीकरण बनने-बिगड़ने की चर्चा हुई, वह इस राज्य की राजनीति का एक रोचक अध्याय है।
पप्पू यादव, जिनका असली नाम राजेश रंजन है, पूर्णिया और कोसी-सीमांचल क्षेत्र में दशकों से एक मजबूत राजनीतिक पहचान रखते हैं। वे पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर उभरे और लालू यादव के समानांतर यादव समाज में अपनी पकड़ बनाने का सपना देखते रहे। उनकी राजनीति का मूल आधार भाजपा विरोध रहा, लेकिन जैसे अक्सर कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यही संभावनाओं का खेल उन्हें 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ले गया।
2015 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में निर्णायक था। एक ओर लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे धुर विरोधी नेता एकजुट हो चुके थे, तो दूसरी ओर भाजपा पहली बार बिहार में अपनी सत्ता की मजबूत दावेदारी पेश कर रही थी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी और पार्टी मानकर चल रही थी कि बिहार की गद्दी अब उसके हाथ में है। इसी दौर में पप्पू यादव ने भाजपा से निकटता बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनकी तुलना लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी से कर डाली। यह बयान चौंकाने वाला था, क्योंकि पप्पू की पूरी राजनीति भाजपा-विरोध की जमीन पर खड़ी थी, लेकिन यह सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपी थी।
दरअसल, लालू यादव ने उसी समय अपने बेटे तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह निर्णय पप्पू के लिए करारा झटका था। वे खुद को यादव समाज में लालू के बाद सबसे बड़ा नेता मानते थे। स्वाभाविक था कि उन्हें लगा कि पार्टी में उनकी प्रासंगिकता कम हो रही है। ऐसे में, वे नए रास्ते तलाशने लगे। भाजपा से नजदीकी इसी खोज का हिस्सा थी। पप्पू यादव और मोदी की मुलाकात की खबर जब सामने आई, तो राजद खेमे में बेचैनी फैल गई। लालू यादव ने उन पर भाजपा से सांठगांठ करने का आरोप लगाया। राजद को डर था कि अगर भाजपा और पप्पू यादव के बीच समझौता हो गया, तो यादव वोटबैंक में सेंध लग सकती है। यही कारण था कि अप्रैल 2015 में पप्पू यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आखिरकार मई 2015 में उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह निष्कासन एक तरह से पप्पू के लिए नया मौका था। उन्होंने तुरंत अपनी नई पार्टी जन अधिकार पार्टी (जाप) का गठन कर लिया और विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए कूद पड़े।
13 अगस्त 2015 को संसद भवन में पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से दूसरी मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह मुलाकात सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं समझी गई। चर्चा यह थी कि भाजपा का एक खेमा कोसी क्षेत्र में पप्पू यादव के प्रभाव का फायदा उठाना चाहता है।
दरअसल, भाजपा को सीमांचल और कोसी इलाके में कभी भी ठोस पकड़ नहीं रही। यह इलाका परंपरागत रूप से राजद और कांग्रेस जैसे दलों का गढ़ रहा। अगर पप्पू जैसे स्थानीय प्रभावशाली नेता भाजपा के साथ आते, तो समीकरण बदल सकते थे। अब सवाल उठता है कि अगर, भाजपा और पप्पू यादव का गठबंधन हो जाता, तो क्या होता? 2015 के चुनाव में महागठबंधन राजद-नीतीश-कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और भाजपा को करारी हार मिली। राजद ने 80 सीटें, जदयू ने 71 सीटें और कांग्रेस ने 27 सीटें जीतीं। दूसरी ओर, भाजपा महज 53 सीटों पर सिमट गई। इस परिदृश्य में अगर, पप्पू यादव भाजपा के साथ होते, तो कोसी और सीमांचल के कई सीटों पर मुकाबला अलग हो सकता था। यादव वोटों में भाजपा को कुछ प्रतिशत का इजाफा मिलता और भाजपा की सीटें 70-80 तक पहुंच सकती थीं। ऐसे में, नीतीश-लालू गठबंधन की जीत इतनी सहज नहीं होती, लेकिन राजनीति में छवि और स्वीकार्यता भी अहम होती है। भाजपा ने यह सोचकर पप्पू से दूरी बनाए रखी कि उनकी छवि बाहुबली और बागी नेता की है, जिससे पार्टी के शहरी और मध्यमवर्गीय वोटरों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नतीजा यह हुआ कि दोनों ही हार गए, पप्पू अपनी पार्टी की एक भी सीट नहीं जीत पाए और भाजपा अपनी पिछली स्थिति से भी नीचे चली गई।
यह पूरा घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि राजनीति सिर्फ अंकगणित नहीं है, बल्कि भावनाओं और छवियों का भी खेल है। पप्पू यादव अपनी महत्वाकांक्षा में भाजपा के करीब जाने को तैयार थे, लेकिन भाजपा अपनी राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए उनके साथ नहीं गई। भाजपा की दुविधा यह थी कि वह यादव वोटबैंक में सेंध लगाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए पप्पू को स्वीकार करना उसके लिए जोखिम भरा था। वहीं, पप्पू को लगा कि भाजपा से गठबंधन उन्हें लालू यादव का सीधा विकल्प बना सकता है। दोनों की इच्छाएं मेल खाती थीं, लेकिन भरोसे और छवि के सवाल पर बात बिगड़ गई।
अगर, उस समय भाजपा और पप्पू यादव का गठबंधन हो जाता, तो बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकती थी।
महागठबंधन की जीत इतनी बड़ी न होती, भाजपा का मनोबल ऊंचा रहता और शायद नीतीश कुमार की वापसी की कहानी कुछ और होती, लेकिन राजनीति में अगर का कोई महत्व नहीं होता। जो हुआ, वही इतिहास बनता है।
2015 का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। पप्पू यादव, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ अपना राजनीतिक करियर खड़ा किया था, वही भाजपा से नजदीकी बढ़ाने लगे। दूसरी ओर भाजपा, जो खुद को नीति और सिद्धांत की पार्टी कहती है, उसने भी पप्पू के साथ संभावित तालमेल पर विचार किया।
लेकिन अंततः यह गठबंधन न हो सका और दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। यह घटना बिहार की राजनीति के उस अनकहे नियम को फिर साबित करती है कि यहां की राजनीति में सबकुछ संभव है, लेकिन हर संभावना अंत तक जाकर वास्तविकता नहीं बनती। आज, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा ने पप्पू यादव के साथ गठबंधन करके कोई ऐतिहासिक गलती टाली, या फिर उसने अपने लिए एक बड़ा अवसर खो दिया? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है।