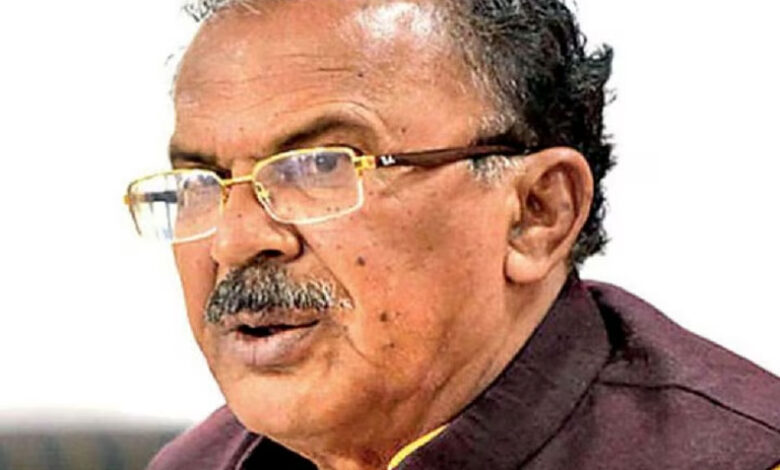
वासुदेव देवनानी
शिक्षा मानव जीवन का आधार है। यह केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि संस्कार, नैतिकता और समाज की प्रगति का वास्तविक स्तंभ है। शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। इस संदर्भ में मेरा यह कथन कि “मैं भी एक शिक्षक हूँ” केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। मैंने अपने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सदैव यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी क्षण, किसी न किसी रूप में एक शिक्षक होता है।
प्राचीन भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। “गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः” यह श्लोक स्पष्ट करता है कि गुरु को सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के समान दर्जा दिया गया है परंतु मेरा यह दृष्टिकोण केवल पारंपरिक गुरु तक सीमित नहीं है। मेरा मानना है कि माँ जीवन का पहला पाठ पढ़ाती है, वह पहली शिक्षक है। पिता अपने बच्चों को संस्कार देता है, वह भी एक शिक्षक है। मित्र सही मार्गदर्शन करता है, वह भी शिक्षक है। अनुभव हमें जीवन का सबक सिखाते हैं, वे भी शिक्षक हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि “मैं भी एक शिक्षक हूँ” क्योंकि हर इंसान अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों को सिखाता है। “मैं भी एक शिक्षक हूँ” का वास्तविक अर्थ यही है कि हम सभी में एक शिक्षक छुपा हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें।समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे आएं। बच्चों को केवल किताबें ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाएं। मेरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में रहकर भी मैंने शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जीवन और कार्य इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है ।
राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने और अब राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष रहने के बावजूद मैंने हमेशा शिक्षा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु माना है। राजनीति में आने से पहलें मैं स्वयं शिक्षक रहा। आज जिस तकनीकी शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है, मैं उसी विषय से जुड़ा हुआ था। मैं देश के सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश राजस्थान का दो बार शिक्षा मंत्री भी रहा। राजस्थान का शिक्षा मन्त्री रहते हुए मैंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनका असर आज भी दिखाई देता है। मैंने राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार किया और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में महापुरुषों, संतों और स्वतंत्रता सेनानियों को शामिल कराया। जिसमें महाराणा प्रताप महान पाठ को शामिल कराना प्रमुख था क्योंकि मेरा प्रारंभ से ही मानना था कि अकबर महान पाठ पढ़ाना सही नहीं है। यह हमारे महान इतिहास का अपमान है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर और अन्य कई महापुरुषों और भारतीय संस्कृति से जुड़े पाठ स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराये। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि प्रेरणा और आदर्श प्रदान करना था। संस्कृत को प्रोत्साहन देने के क्रम में मैंने संस्कृत भाषा को प्राचीन भारतीय ज्ञान की कुंजी मानते हुए इसे विद्यालय स्तर पर बढ़ावा दिया। स्मार्ट स्कूल योजना के अन्तर्गत शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल क्लासरूम, ई-कंटेंट और प्रोजेक्टर आधारित पढ़ाई शुरू कराई। विद्यालय अनुशासन पर बल देते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। ‘पढ़ो राजस्थान’ जैसी योजनाओं से शिक्षा में नवाचार लाने का कार्य किया। नैतिक शिक्षा पर बल देने से विद्यार्थियों के नेतृत्व में यह प्रयास हुआ कि विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि व्यवहार और सामाजिक उत्तरदायित्व में भी श्रेष्ठ बनें। मेरा मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। प्रौद्योगिकी और आधुनिकता का समावेश शिक्षा को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। अनुशासन और मूल्य आधारित शिक्षा ही समाज को सही दिशा देती है।
मेरे लिए “मैं भी एक शिक्षक हूँ” यह वाक्य जीवन का मूल मंत्र है। राजनीति में रहते हुए भी मैंने स्वयं को समाज का शिक्षक माना हैं। क्योंकि जीवन स्वयं सबसे बड़ा विद्यालय है। अनुभव सबसे बड़ी पाठ्य पुस्तक है। हर व्यक्ति जो कुछ सीखता है, उसे समाज के साथ साझा करना उसका कर्तव्य है। इस दृष्टिकोण से हर किसी को अपने आपको शिक्षक और एक निरंतर सीखने वाला और सिखाने वाला इन्सान मानना चाहिए। आज के समय में जब शिक्षा को केवल डिग्री और रोजगार तक सीमित कर दिया गया है, मेरा यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है कि यदि समाज को सशक्त बनाना है, तो शिक्षा में संस्कार और संस्कृति को स्थान देना होगा। शिक्षक को केवल अध्यापक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और जीवन निर्माता होना चाहिए। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य समग्र विकास होना चाहिए, न कि केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना। “मैं भी एक शिक्षक हूँ” केवल एक विचार या भाषण नहीं है। यह एक जीवन दृष्टि है। शिक्षक होना किसी पद, वेतन या संस्था से बंधा हुआ कार्य नहीं है बल्कि, जब भी हम किसी को सही मार्ग दिखाते हैं, अनुभव साझा करते हैं और समाज को शिक्षित करते हैं, तब हम शिक्षक बन जाते हैं। वास्तविकता में हर व्यक्ति शिक्षक है और हर क्षण शिक्षा का अवसर है। इसलिए यह कथन हमारे हृदय और मन में गहराई से छू जाना चाहिए कि “मैं भी एक शिक्षक हूँ।” क्योंकि इसी वाक्य में जीवन की सार्थकता छुपी हुई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों, “मन की बात” और शिक्षक दिवस जैसे अवसरों पर शिक्षा और शिक्षक पर विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, जीवन निर्माण है। शिक्षा का लक्ष्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बच्चों के चरित्र, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को विकसित करने वाली होनी चाहिए। नई पीढ़ी को भविष्य के अनुरूप तैयार करने के लिए आज की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता की ओर ले जाए। शिक्षा में भारतीयता और आधुनिकता का संतुलन होना चाहिए। शिक्षा में भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक विज्ञान और तकनीक को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति इसी सोच का परिणाम है, जो 21वीं सदी के भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा अधिक लचीली, बहुविषयक और कौशल आधारित हो। इसमें मातृभाषा में पढ़ाई, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी उपयोग पर विशेष बल दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर कहते है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, लेकिन शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और आदर्श प्रस्तुत करने वाले के रूप में कभी कम नहीं हो सकती। गुरु केवल पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि जीवन को गढ़ने वाला होता है। एक अच्छा शिक्षक पूरी जिंदगी विद्यार्थियों के मन-मस्तिष्क पर छाप छोड़ता है।
शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। यदि शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त होगी, तभी समाज और देश का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बन सकता है। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, परंतु यह भी सच है कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, पक्षपात और अपारदर्शिता जैसी चुनौतियाँ समय-समय पर सामने आती रही हैं। इन चुनौतियों को दूर करके ही एक ऐसी शिक्षा प्रणाली आवश्यक है जो वास्तव में न्यायसंगत, निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान करने वाली हो। प्रतिभाओं को उचित अवसर देना जरूरी है क्योंकि जब प्रवेश, नियुक्ति या परीक्षा में भ्रष्टाचार होता है तो योग्य छात्र-शिक्षक पीछे छूट जाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा से देश को योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासक और वैज्ञानिक मिलेंगे। इसी प्रकार रिश्वत या सिफ़ारिश से प्रवेश और पद पाना गरीब और ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय है। यदि शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी होगी तो छात्रों, अभिभावकों और समाज का इसमें विश्वास बढ़ेगा।
शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, भर्ती और वित्तीय लेन-देन पूरी तरह ऑनलाइन और ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित होंने चाहिए। शिक्षा विभाग की नीतियाँ, बजट, खर्च और भर्ती प्रक्रिया सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हों। शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति योग्यता आधारित मूल्यांकन पर हो, छात्रों की राय को भी महत्व मिले। पेपर लीक, फर्जीवाड़ा या रिश्वत के मामलों में शीघ्र और कठोर दंड सुनिश्चित होंने चाहिए। अभिभावक संघ, स्थानीय निकाय और नागरिक समाज को विद्यालयों की गुणवत्ता और प्रशासन में भागीदारी दी जानी चाहिए जिससे योग्य छात्रों को बिना भेदभाव अवसर मिलेगा और शिक्षा पर समाज का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और शोधकर्ता तैयार होंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए ईमानदार और कुशल नेतृत्व विकसित होगा। कुल मिला कर, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही नए भारत की नींव है। यह केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि शिक्षक, छात्र, अभिभावक और समाज सभी की संयुक्त जिम्मेदारी से संभव है।
इसी प्रकार एआई और तकनीकी कन्सल्टिंग को अगर शाला दर्पण और शाला दर्शन जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए तो शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सशक्त और उत्तरदायी बनाया जा सकता है। साथ ही यह भारत में शिक्षा गवर्नेंस का एक आदर्श मॉडल भी बन सकता है। शिक्षा केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम होनी चाहिए। । आज की पीढ़ी में छात्र (स्कूल स्तर) और युवा (कॉलेज/विश्वविद्यालय, पेशेवर या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय वर्ग) समाज के सबसे ऊर्जावान हिस्से हैं। यदि इन दोनों के बीच संवाद और अनुभवों का आदान-प्रदान नियमित रूप से हो, तो शिक्षा और अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और सार्थक बन सकती है। छात्रों और युवाओं का संवाद केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी मजबूत बनानें में सहायक है।
शिक्षक समाज के प्रति बनें संवेदनशील
शिक्षक जब अपने दायित्वों को निष्ठा से निभाते हुए समाज की पीड़ा, समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं, तभी वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की शक्ति में बदल पाते हैं। मैंने शिक्षक रहते हुए कुछ ऐसे प्रयोग करने का प्रयास किया जिसका छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । मैं अपने छात्रों के एक दल को उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में लेकर गया और उनसें कहा कि वे दस दिनों तक इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर ग्रामीणों के साथ रहें और वे जैसा जीवन जीते है उसे देखें, तथा वैसा ही जीवन जीएं । वे जैसा खातें है वह खाना खायें तथा वैसा ही पानी पीयें। दस दिन बाद जब छात्रों का यह दल लौट कर वापस आया तो उनकी आँखों में आँसू थे। छात्रों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हों रहा कि ऐसी भी गरीबी कहीं हों सकती है? उन्होंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से जो देखा वह कल्पना से परे है ।
इसी प्रकार जब मैं उदयपुर के विद्या भवन संस्थान में तकनीकी शिक्षक था तब गाँवों में दौरा करते समय ग्रामीण महिलाओं को पत्थर की घटी पर गैहूँ और अन्य धान पिसते हुए देखा और उनसे बात की तो ज्ञात हुआ कि उन्हें परिश्रम भरें इस कार्य से कमर में दर्द आदि की शिकायत रहती है। इस पर विचार आया कि उनकी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए? फिर हमने अपने तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग करते हुए उनकी घटी के साथ एक बेरिंग लगा दी ताकि घटी स्मूथ गति से चल सकें तथा इन महिलाओं को घटी चलाने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़े। इस प्रकार उनकी समस्या का समाधान हो गया लेकिन कुछ दिनों पश्चात उन्होंने एक समस्या और बता दी कि घटी के साथ बेरिंग लगने से बहुत आसानी हो गई है लेकिन आटा बहुत महिन पिसने लगा है जबकि कई बार उन्हें मोटा आटा भी चाहिये । इस पर बेरिंग के साथ एक स्प्रिंग लगाने से उनकी वह समस्या भी सुलझ गई । उन दिनों में जब ग्राइंडर और मिक्सी जैसी सुविधाएं नहीं थी ऐसे में इस तकनीकी से उन्हें बहुत राहत मिली । इस प्रकार समाज के लोगों के प्रति संवेदनशीलता का भाव रख कर शिक्षक उनकी कई समस्याओं का तत्काल समाधान कर सकता है I
(लेखक श्री वासुदेव देवनानी राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष है)







