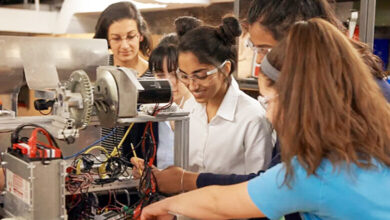संजय सक्सेना
भारतीय राजनीति में वंशवाद का मुद्दा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एलईडब्लूय) द्वारा 12 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट ने इस पुरानी समस्या को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में देशभर के 5,204 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की गहन पड़ताल की गई और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि हर पांच में से एक नेता, यानी लगभग 21 प्रतिशत जनप्रतिनिधि, राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की कमजोर होती नींव का प्रतीक है। लोकसभा में यह आंकड़ा और भी अधिक, 31 प्रतिशत तक पहुँच गया है। राज्यसभा में 21 प्रतिशत, राज्य विधानसभाओं में 20 प्रतिशत और विधान परिषदों में 22 प्रतिशत नेता परिवारवाद की छाया में राजनीति कर रहे हैं।परिवारवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन युवा नेताओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है जिनके परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार, राष्ट्रीय जनता दल में लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव,समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव, तमिलनाडु में करुणानिधि की वंशवाद वाली सियासत, महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे,रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान को,पंजाब में बादल परिवार,हरियाणा में चौटाला परिवार तो बसपा में मायावती के बाद उनके भतीजे आकाश, पश्मिच बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही उत्तराधिकारी की कुर्सी क्यों मिलती है। क्या पार्टी में परिवार से बाहर के नेताओं की कमी रहती है।
बात राष्ट्रीय दलों से शुरू की जाये तो इसमें कांग्रेस सबसे आगे है। नेहरू-गांधी परिवार की विरासत यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नाम सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में वंशवाद का प्रतीक बन चुके हैं। कांग्रेस के कुल नेताओं में 32 प्रतिशत परिवारवादी हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत, भाजपा में 17 प्रतिशत और वामपंथी दल सीपीआई(एम) में केवल 8 प्रतिशत है। इसके विपरीत, तृणमूल कांग्रेस और एआईएडीएमके जैसी दलों में यह प्रतिशत काफी कम है दृ 10 और 4 प्रतिशत। इसका कारण है कि ये दल मजबूत संगठन और काडर-आधारित संरचना पर विश्वास करते हैं, जिससे नए नेताओं को मौका मिल पाता है।
क्षेत्रीय दलों की स्थिति और भी चिंताजनक है। एनसीपी (शरद पवार गुट) और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 42-42 प्रतिशत नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। वाईएसआर कांग्रेस में यह आंकड़ा 38 प्रतिशत और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में 36 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत में भी परिवारवाद अब राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुका है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसी के जगन मोहन रेड्डी इसके जीते-जागते उदाहरण हैं।
राज्यवार आंकड़े भी चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश वंशवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। 604 जनप्रतिनिधियों में 141 (23 प्रतिशत) परिवारवादी हैं। लोकसभा में यूपी के 28 सांसदों में राहुल गांधी (रायबरेली), अखिलेश यादव (कन्नौज), अनुप्रिया पटेल (अपना दल), जितिन प्रसाद (पीलीभीत) और जयंत चौधरी (रालोद) शामिल हैं। राज्यसभा में रामगोपाल यादव, आरपीएन सिंह और नीरज शेखर जैसे नामों ने यह साबित किया कि यहां वंशवाद गहराई तक फैला हुआ है। समाजवादी पार्टी के 161 नेताओं में 48 (30 प्रतिशत) और भाजपा के 17 प्रतिशत नेता वंशवादी हैं।
अनुपात में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 255 नेताओं में 86 (34 प्रतिशत) परिवारवादी हैं। महाराष्ट्र में 403 में 129 (32 प्रतिशत), बिहार में 360 में 96 (27 प्रतिशत), कर्नाटक में 326 में 94 (29 प्रतिशत) और असम में केवल 13 (9 प्रतिशत) नेता परिवारवादी हैं। तमिलनाडु (15 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (9 प्रतिशत) में काडर-आधारित दलों की मजबूती के कारण यह आंकड़ा कम है। झारखंड और हिमाचल प्रदेश में यह क्रमशः 28 और 27 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से यह साफ़ होता है कि बड़े और प्रभावशाली राज्यों में वंशवाद लोकतंत्र को निगलता जा रहा है।
महिलाओं के मामले में स्थिति और भी गंभीर है। कुल 539 महिला सांसदों-विधायकों में 47 प्रतिशत (251) नेता सियासी परिवारों से हैं, जबकि पुरुष नेताओं में यह आंकड़ा केवल 18 प्रतिशत (856/4,665) है। उत्तर प्रदेश में 69 महिला नेताओं में से 29 (42 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 39 में 27 (69 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश में 29 में 20 (69 प्रतिशत) और बिहार में 44 में 25 (57 प्रतिशत) महिला नेता परिवारवाद से आते हैं। तेलंगाना में यह आंकड़ा 64 प्रतिशत और गोवा-पुडुच्चेरी में 100 प्रतिशत है। भाजपा में 41 प्रतिशत और कांग्रेस में 53 प्रतिशत महिला नेता परिवार से हैं। सपा में यह संख्या 67 प्रतिशत है। इसका मतलब यह साफ़ है कि महिलाओं को राजनीति में लाने का मार्ग परिवारवाद के माध्यम से ही संभव होता है, जबकि गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के लिए अवसर सीमित रह जाते हैं।
वंशवाद केवल बड़े दलों तक सीमित नहीं है। छोटे और अपंजीकृत दलों के 87 नेताओं में से 21 (24 प्रतिशत) वंशवादी हैं। नौ दल पूरी तरह से परिवार आधारित हैं। निर्दलीयों में 94 में से 23 (24 प्रतिशत) नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह दिखाता है कि वंशवाद हर स्तर पर गहरा चुका है और इसका दायरा न केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों तक, बल्कि स्थानीय राजनीति तक फैल चुका है।
एडीआर की रिपोर्ट ने इसके चार प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण है चुनावों का महंगा होना। एक औसत उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में दल उन लोगों को टिकट देते हैं, जिनके पास पैसा और नेटवर्क हो। दूसरा कारण है दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी नहीं होता और परिवार हावी हो जाते हैं। तीसरा कारण ‘जीतने की क्षमता’ का तर्क है। राजनीतिक परिवारों के नाम और नेटवर्क वोट दिलाने में मदद करते हैं। चौथा कारण सामाजिक न्याय के नाम पर बने दलों में भी परिवारवाद का प्रभाव है। सपा, आरजेडी जैसे दलों में परिवार ही राजनीति का केंद्र बन चुके हैं।
इस रिपोर्ट में वंशवाद को रोकने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक चुनाव और गुप्त मतदान के माध्यम से पद चयन और टिकट वितरण में पारदर्शिता लानी चाहिए। महिलाओं के लिए एक-तिहाई टिकट अनिवार्य की जानी चाहिए और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो। महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना होगा और प्रॉक्सी या टोकन उम्मीदवारों की नीति समाप्त करनी होगी। उम्मीदवारों को परिवार की शक्ति के बजाय योग्यता के आधार पर चयनित किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दलों को अपने चयन मानदंड सार्वजनिक करने होंगे और दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। चुनाव खर्च पर सख्त सीमा लगाई जानी चाहिए। युवाओं को भी मौके मिलें, गैर-वंशवादी उम्मीदवारों और महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए और मतदाताओं को वंशवाद के नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए।
वंशवाद लोकतंत्र को धीरे-धीरे खोखला कर रहा है। यह नई प्रतिभाओं को दबाता है, जवाबदेही को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करता है। एडीआर की यह रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सभी दल कांग्रेस, भाजपा, सपा, टीडीपी को अपनी कमियों को सुधारना होगा। नेपाल में जेन जेड ने नेपोटिज़्म के खिलाफ आंदोलन कर सरकार तक गिरा दी। भारत के युवा भी अगर जागरूक हों, तो बदलाव की राह बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गैर-राजनीतिक युवाओं को मौका देने की बात कही है, लेकिन जमीनी बदलाव अभी धीमा है। सवाल यह है कि क्या हम योग्यता पर आधारित लोकतंत्र चाहते हैं या वंशवाद के खेल को जारी रखना चाहते हैं? जवाब आने वाला समय ही देगा।