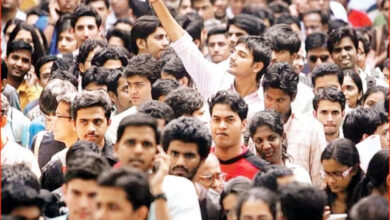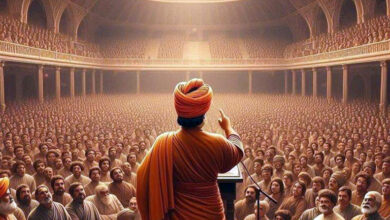सोनम लववंशी
यह सच है कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वंशवाद की परंपरा इसकी आत्मा को खोखला करती जा रही है। यह परंपरा किसी एक राजनीतिक दल या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में फैली हुई है। एक ओर लोकतंत्र अवसर की समानता और प्रतिनिधित्व की विविधता का वादा करता है, तो दूसरी ओर वंशवाद की यह बेल आमजन को हाशिये पर धकेलते हुए सत्ता को चुनिंदा घरानों के इर्द-गिर्द केंद्रित कर देती है। एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की हालिया रिपोर्ट इस सच्चाई को और स्पष्ट करती है। देश के कुल 5,204 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया कि इनमें से 1,107 यानी करीब 21 प्रतिशत प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि वंशवादी है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि लोकसभा में इनकी हिस्सेदारी 31 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर तीसरा सांसद किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आता है।
अगर दलों की बात करें तो कांग्रेस इस दौड़ में सबसे आगे दिखाई देती है। कांग्रेस के कुल प्रतिनिधियों में से 32 प्रतिशत नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस में अब भी राजनीति में प्रवेश का सबसे आसान टिकट वंश परंपरा ही है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी, जो अक्सर वंशवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, उसके भी 18 प्रतिशत प्रतिनिधि वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। वामपंथी दलों में यह आंकड़ा 8 प्रतिशत है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वहां वंशवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है, बल्कि यह केवल एक अलग तरह के संगठनात्मक ढांचे के कारण सीमित है। यदि सदनों की बात करें तो राज्य विधानसभाओं में 20 प्रतिशत, राज्यसभा में 22 प्रतिशत और विधानपरिषदों में 22 प्रतिशत प्रतिनिधि राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाती है कि चाहे संसद हो या राज्य का विधानमंडल, वंशवाद हर जगह अपनी गहरी पकड़ बनाए हुए है। कुछ राज्यों में यह प्रवृत्ति और भी गहरी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में वंशवादी प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश से 141 ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि वंशवादी है, जबकि महाराष्ट्र से 129, बिहार से 96 और कर्नाटक से 94 प्रतिनिधि इसी श्रेणी में आते हैं।
लोकतंत्र की आत्मा समान अवसर और समान अधिकार पर आधारित है। संविधान ने यह आश्वासन दिया है कि हर नागरिक को राजनीति में भाग लेने और सत्ता तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब राजनीति पर वंशवाद का कब्जा बढ़ता है तो यह अवसर केवल चुनिंदा परिवारों तक सीमित हो जाता है। आम युवाओं या नए चेहरों के लिए राजनीति में प्रवेश की राह ओर भी कठिन हो जाती है। दलों में टिकट वितरण का आधार अक्सर योग्यता या जनाधार न होकर पारिवारिक पहचान बन जाता है। इससे राजनीति में नई सोच और नई ऊर्जा का प्रवेश बाधित होता है। यह प्रवृत्ति केवल अवसर की असमानता ही पैदा नहीं करती, लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। जब जनता देखती है कि चुनावी मैदान में अधिकतर उम्मीदवार उन्हीं परिवारों से आते हैं जो दशकों से सत्ता पर काबिज हैं, तो उसके भीतर यह भावना पनपती है कि राजनीति एक बंद दरवाजा है, जहां आम आदमी की पहुंच नामुमकिन है। इस तरह लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार स्तंभ जनप्रतिनिधित्व धीरे-धीरे खोखला हो जाता है।
वंशवाद का असर केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहता, यह नीति-निर्माण और शासन की दिशा को भी प्रभावित करता है। जब नेतृत्व विरासत में मिलने लगता है तो उसके भीतर जवाबदेही और संघर्षशीलता का भाव कमजोर हो जाता है। ऐसे नेता जिनका उदय केवल परिवार की पहचान के कारण हुआ हो, उनके लिए जनता की समस्याओं को गहराई से समझना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना प्रायः कठिन हो जाता है। वे सत्ता को अपने अधिकार की तरह देखना शुरू कर देते हैं, न कि जनता की सेवा का माध्यम। यही कारण है कि वंशवाद लोकतंत्र की उस मूल भावना के विपरीत खड़ा है जिसमें सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता मानी गई है।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो वंशवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता। यह समाज में असमानताओं को और गहरा करता है। जब सत्ता कुछ परिवारों तक सीमित होती है, तो इससे सामाजिक अन्याय की जड़ें और मजबूत होती हैं। अवसर की समानता का सपना टूटता है और समाज में यह संदेश जाता है कि चाहे शिक्षा, क्षमता और प्रतिभा कितनी भी हो, अगर परिवारिक पहचान नहीं है तो राजनीति में स्थान पाना मुश्किल है। यह व्यवस्था उस समावेशी समाज की राह में बाधा बनती है जिसकी कल्पना संविधान ने की थी। यह भी विचारणीय है कि वंशवाद केवल वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता है। जब अगली पीढ़ी के सामने राजनीति का रास्ता पहले से तय हो, तो वे सत्ता को संघर्ष की बजाय विरासत मानने लगते हैं। यह लोकतंत्र को स्थायी नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति है। इसके विपरीत, अगर राजनीति योग्यता और जनसमर्थन पर आधारित हो, तो उसमें संघर्षशील, जनता से जुड़े और जवाबदेह नेता उभरते हैं।
इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल अपने टिकट वितरण में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दें। जनता को भी इस प्रवृत्ति को पहचानकर ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देनी होगी जिनकी राजनीति उनकी अपनी मेहनत और जनता से जुड़ाव के कारण बनी हो। चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को भी इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हों। भारत का लोकतंत्र अपनी विविधता और समावेशी प्रकृति के कारण दुनिया में अलग पहचान रखता है। लेकिन अगर वंशवाद की बेल इसी तरह फैलती रही तो यह लोकतंत्र को भीतर से कमजोर कर देगी। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ तभी साकार होगा जब राजनीति हर नागरिक के लिए खुला मंच बने, न कि कुछ परिवारों की निजी जागीर। वंशवाद के खिलाफ यह संघर्ष केवल राजनीतिक सुधार का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का संघर्ष है। आख़िरकार, लोकतंत्र की ताकत उसकी जनता होती है। अगर जनता ही अवसर की समता और समान प्रतिनिधित्व से वंचित कर दी जाए तो यह लोकतंत्र के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न है। इसलिए वंशवाद को समाप्त करना केवल एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा को बचाने की अनिवार्यता है। यही वह राह है जो भारत को एक वास्तविक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा सकती है।