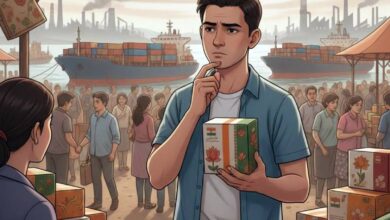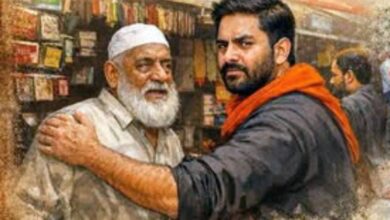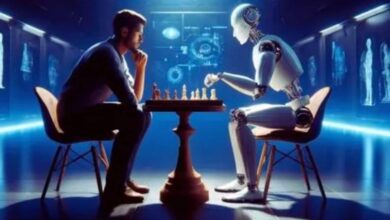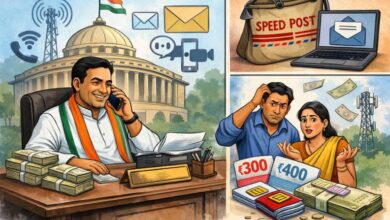नृपेन्द्र अभिषेक ‘नृप’
कूटनीति एक ऐसी अंतर्धारा है जो राष्ट्रों के संबंधों को संयम, समझदारी और दीर्घदृष्टि से सिंचित करती है। सीमाओं के पार व्याप्त तनाव, वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताएँ और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के बीच यदि कोई राष्ट्र स्थिरता, संतुलन और परिपक्वता का उदाहरण बनकर उभरता है, तो निःसंदेह यह उसकी कुशल विदेश नीति का प्रमाण है। भारत, अपने पारंपरिक सिद्धांतों- ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को केंद्र में रखते हुए, एक ऐसे कूटनीतिक पथ का निर्माण कर रहा है, जो न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी योगदान देता है। हाल के वर्षों में भारत ने चीन, अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियों से संबंधों में सामंजस्य साधते हुए जिस दूरदर्शिता और संतुलन का परिचय दिया है, वह सराहना के योग्य है। विशेष रूप से भारत-चीन संबंधों में हालिया नरमी और संवाद के नए दौर ने यह संकेत दिया है कि अतीत की खटास को पीछे छोड़, दोनों राष्ट्र परिपक्वता के साथ आगे बढ़ने को तत्पर हैं।
भारत-चीन संबंध: खटास से विश्वास की ओर
भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएँ हैं, जिनके बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। किंतु समकालीन संदर्भ में दोनों देशों के बीच रिश्ते विशेष रूप से 2020 के गलवान संघर्ष के बाद जटिल हो गए थे। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के बलिदान ने द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी तल्ख़ी पैदा कर दी थी, जिसे सामान्य करना आसान नहीं था। इसके बाद सीमा पर गश्त, चरागाही गतिविधियों, और सैनिकों की तैनाती पर दोनों देशों में तनातनी बनी रही। परंतु वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कज़ान (रूस) में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई वार्ता ने इस दिशा में एक नई शुरुआत का संकेत दिया।
साथ ही हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बीजिंग यात्रा और चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ हुई बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि अब दोनों देश ‘सामान्यता की बहाली’ के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस यात्रा में कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः प्रारंभ होने की चर्चा तथा एलएसी पर तनाव कम करने की प्रतिबद्धता जैसे सकारात्मक संकेत उभर कर सामने आए। भारत की ओर से विदेश मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बहाल करना और शांति बनाए रखना दोनों देशों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं चीनी नेतृत्व ने भी भारत के प्रति ‘नए दृष्टिकोण’ और ‘पारस्परिक सम्मान’ की बात कही।
कैलाश मानसरोवर यात्रा, न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास का भी प्रतीक रही है। पिछले पाँच वर्षों से यह यात्रा निलंबित थी, लेकिन अब इसे पुनः प्रारंभ करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं। भारत ने इस पहल की सराहना की है और इसे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की दिशा में एक भावनात्मक एवं सांस्कृतिक पुल के रूप में देखा जा रहा है। यह पहल बताती है कि दोनों देशों में पारस्परिक समझ को सुदृढ़ करने की भावना पुनः जागृत हो रही है।
भारत की संतुलित विदेश नीति: अमेरिका, चीन और रूस के मध्य संतुलन का अद्भुत उदाहरण
भारत की विदेश नीति का मौजूदा स्वरूप “सार्वभौमिक संतुलन” की नीति का अनुपम उदाहरण है। भारत ने बीते वर्षों में अमेरिका, चीन और रूस जैसे तीनों वैश्विक ध्रुवों से अपनी साझेदारी को इस प्रकार साधा है कि किसी एक ध्रुव पर निर्भरता न बने और न ही किसी एक से दूरी बने। यह नीति विशेष रूप से तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीकी, और सैन्य तनाव चरम पर हो, और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों से अलग-थलग पड़ा हो।
भारत ने रूस से सस्ते तेल और रक्षा उपकरण खरीदने की परंपरा को जारी रखा, तो वहीं अमेरिका से रणनीतिक, तकनीकी और डिजिटल साझेदारी को भी प्रगाढ़ किया। क्वाड, आई. पी. ई. एफ़. (IPEF) और इंडो- पैसिफिक रणनीतियों में भारत की सक्रिय भागीदारी यह संकेत देती है कि भारत वैश्विक मंचों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। परंतु साथ ही ब्रिक्स, एस. सी. ओ. (SCO) और रूस के साथ ऊर्जा सहयोग को बनाए रखना यह दर्शाता है कि भारत ने तटस्थता की एक संतुलित भूमि खोज निकाली है।
चीन के प्रति सख्त परंतु व्यावहारिक रुख
भारत ने चीन के प्रति दोहरी नीति अपनाई है-एक ओर सीमा पर आक्रामकता का ठोस जवाब दिया है, वहीं दूसरी ओर संवाद और कूटनीतिक खिड़कियाँ खुली रखी हैं। 2024 में बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जिस स्पष्टता से संयुक्त घोषणापत्र में आतंकवाद का उल्लेख कराया, वह कूटनीतिक विजय रही। ब्रिक्स में भारत के प्रयासों से पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट निंदा दर्ज की गई, जिसमें पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों का संकेत भी था। इसी बैठक में भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को “दक्षिण तिब्बत” बताने और मानचित्र विवाद पर भी तीव्र प्रतिक्रिया दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी सीमाओं, संप्रभुता और आत्मगौरव पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।
भारत और चीन के संबंधों में ताइवान, दलाई लामा, ब्रह्मपुत्र नदी के जल विवाद और जम्मू-कश्मीर में चीन-पाक गठजोड़ जैसे मुद्दे दीर्घकालिक तनाव के कारक हैं। भारत ने इन सभी विषयों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। चीन यदि ‘वन चाइना पॉलिसी’ की पुनः पुष्टि चाहता है, तो उसे भी ‘वन इंडिया’ नीति का सम्मान करना होगा अर्थात अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, और जम्मू-कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं और उन पर चीन की कोई टिप्पणी या गतिविधि अस्वीकार्य है।
चीन की रणनीति और भारत की सतर्कता
बीते कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी को आक्रामक रूप से बढ़ाया है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में उसके निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ, बंदरगाह निर्माण, तथा कर्ज के जाल ने भारत को सजग कर दिया है। भारत ने भी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘इंडो-पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन रणनीति’ के माध्यम से चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की ‘एक्सक्लूसिव’ सोच की तुलना में भारत की ‘समावेशी’ विदेश नीति अधिक व्यावहारिक और स्थायी है। भारत सहयोग और पारदर्शिता में विश्वास करता है, जबकि चीन अनेक अवसरों पर अपारदर्शिता, दबाव और संदेहास्पद रणनीतियों का सहारा लेता है।
आर्थिक सहयोग और तकनीकी संतुलन
भारत-चीन व्यापार संबंधों में असमानता एक बड़ी चुनौती है। चीन से भारत का आयात बहुत अधिक है, जबकि निर्यात सीमित है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, फार्मा और उच्च तकनीक क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है। साथ ही व्यापार संतुलन सुधारने के लिए विविध बाजारों की तलाश की है। दूसरी ओर, भारत ने अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के साथ तकनीकी सहयोग और निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी मजबूत हो सके।
भारत की वैश्विक कूटनीति में ‘संवेदनशील सतर्कता’ की नीति
भारत की विदेश नीति में एक विशेष गुण उभर कर सामने आया है जिसे ‘संवेदनशील सतर्कता’ (सेंसिटिव विजिलेंस) कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि भारत अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव को बनाए रखते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। यह नीति ना तो एकपक्षीय झुकाव में विश्वास करती है, और ना ही भावनात्मक प्रतिक्रिया में बहती है। भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में यह नीति विशेष रूप से सार्थक सिद्ध हुई है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन के साथ सहयोग चाहता है, परंतु यह सहयोग समानता, पारस्परिक सम्मान और पारदर्शिता की बुनियाद पर ही टिकेगा। भारत यह भी जानता है कि चीन की विस्तारवादी नीति और रणनीतिक आक्रामकता को सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीतिक धैर्य और बहुस्तरीय गठजोड़ से संतुलित किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ भी अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है।
उभरते एशिया में भारत की भूमिका:
21वीं सदी को ‘एशियाई सदी’ कहा जा रहा है और इस सदी में भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा भी होगी और साझेदारी की संभावनाएँ भी। चीन जहां अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर प्रभाव जमाना चाहता है, वहीं भारत वैचारिक समावेशिता, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवता-केन्द्रित विकास मॉडल के ज़रिए वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। चीन की बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बी. आर. आई.) जैसी परियोजनाओं में भारत की अनुपस्थिति यह दिखाती है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना चाहता है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक संवाद, क्वाड जैसी संस्थाओं में भागीदारी, और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज़ बनने की भारत की कोशिशें यह संकेत देती हैं कि भारत अब सिर्फ ‘क्षेत्रीय शक्ति’ नहीं, बल्कि ‘ग्लोबल सॉफ्ट पावर’ के रूप में देखा जा रहा है।
समाधान:भारत की संयमित रणनीति
भारत का रुख अब प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, वह समाधान की ओर भी उन्मुख है। चाहे वह यूक्रेन युद्ध पर भारत का संतुलित रुख हो या इस्राइल-हमास संघर्ष के प्रति विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया- भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह वैश्विक तनावों में ‘स्थिरता का स्तंभ’ (पिलर ऑफ स्टेबिलिटी) बनकर उभर सकता है। चीन के साथ सीमा विवादों पर भारत की नीति भी इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है- सीमाओं की रक्षा के लिए शक्ति, लेकिन शांति के लिए संवाद। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बार-बार यह दोहराया है कि “बॉर्डर पर शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की पूर्वशर्त है।” यह वक्तव्य भारतीय नीति की स्पष्टता और आत्मविश्वास को दर्शाता है।
जनमानस में भरोसा: विदेश नीति का जनसंचार पक्ष
भारत की विदेश नीति की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि आज उसका स्वरूप सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आम नागरिकों के मन में भी विश्वास उत्पन्न करती है। गलवान संघर्ष के बाद जब देश में आक्रोश था, तब सरकार ने न केवल सेनाओं को पूरा समर्थन दिया, बल्कि विश्व मंच पर चीन को घेरने का भी प्रयास किया। ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसी पहलें देश को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने के साथ-साथ चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में ठोस कदम थीं। इसके साथ ही, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, अरुणाचल में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, और एलएसी पर बेहतर प्रबंधन जैसे कार्यों ने आम नागरिकों के मन में यह विश्वास जगाया है कि भारत अब ‘न सिर्फ़ सहन करता है, बल्कि सही समय पर सही भाषा में जवाब देना जानता है।’
नवभारत की दिशा: आत्मनिर्भर, आत्मगौरवी, और आत्मनिष्ठ विदेश नीति
आज का भारत उस नवचेतना के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव समाहित हैं। उसकी विदेश नीति ‘गुटनिरपेक्षता’ की पारंपरिक सोच से आगे निकलकर ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ के यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित हो चुकी है। भारत आज अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, जापान, अफ्रीका और मध्य एशिया सभी से अपने हितों के अनुसार सम्बन्ध बनाता है- न किसी के पिछलग्गू बनकर, न किसी के विरुद्ध जाकर। भारत की यह विदेश नीति न केवल वर्तमान वैश्विक संकटों में समाधान खोजने का प्रयास कर रही है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता बना रही है जो शक्ति और शांति के मध्य संतुलन का श्रेष्ठ उदाहरण बन सके।
भारत-चीन संबंधों का सुधार और वैश्विक मंचों पर भारत की संतुलित उपस्थिति यह दर्शाते हैं कि भारत की विदेश नीति अब केवल ‘प्रतिक्रिया’ नहीं, बल्कि ‘रणनीति’ के स्तर पर विकसित हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राजनयिक तंत्र की दूरदृष्टि ने भारत को विश्व राजनीति के केंद्र में स्थापित किया है। यह स्पष्ट है कि भारत अब न तो ‘वेट ऐंड वॉच’ की नीति अपनाता है और न ही ‘बेंड ऐंड ब्लेम’ की रणनीति पर चलता है। वह अब ‘एक्ट एंड एसेस’ यानी कार्रवाई करो और मूल्यांकन करो की नीतिगत सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है- संयम, संवाद और संप्रभुता की त्रयी पर टिका हुआ उसका विवेकपूर्ण, दृढ़ और संतुलित विदेश नीति दृष्टिकोण। यही दृष्टिकोण भारत को 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बनाएगा।