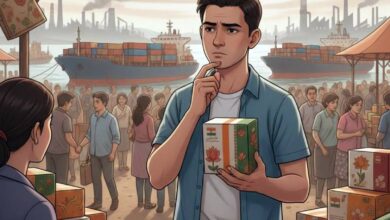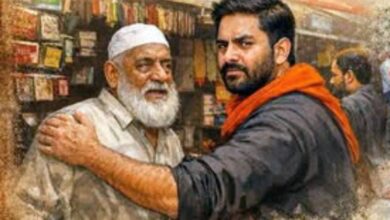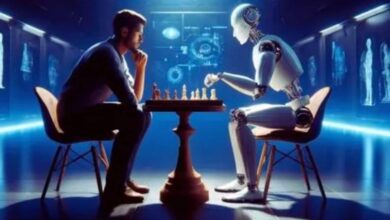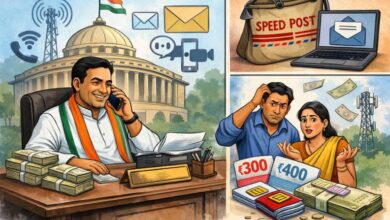प्रो. नीलम महाजन सिंह
पिछले दिनों अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रहारक बयान ने मीडिया में हडकप मचा दी है। इसका एक कारण यह भी है, कि सरकार के प्रवक्ता व भाजपाई बार-बर यह कह रहे हैं कि ‘अमेरिका की ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम में कोई भूमिका नहीं है’। उधर डोनाल्ड ट्रम्प ने अनेकों बार कहा है कि उन्होंने जनरल मुनीर से स्वयं बात कर युद्धविराम करवाया था। इससे दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा बड़ी है। भारत-अमेरिका के बीच बदलते संबंध की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करना कठिन है। अब दोनों देशों का संबंध सिर्फ सामयिक या प्रतीकात्मक नहीं रहा, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में अग्रसर (विशेषकर प्रौद्योगिकी, रक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में) हो रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तय नहीं हुआ। परमाणु अप्रसार संधि (NPT) मानदंड, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, ‘आर्टेमिस समझौते’, खनिज सुरक्षा साझेदारी, महत्त्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हाल के संयुक्त वक्तव्य व सहयोग के लिये नए ढाँचे एक गहरी साझेदारी का संकेत देते हैं। हालाँकि, बाहरी चुनौतियों और उतार-चढ़ाव भरे व्याख्यान के बावजूद, भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की ज़रूरत है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सतत्, दीर्घकालिक सहयोग पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। विकसित हो रही गतिशीलता द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह समय भारत को व्यावहारिक और दूरदर्शी कूटनीति के माध्यम से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने का आह्वान करता है। प्रारंभिक वर्ष (1947-1960) शीत युद्ध की तनावपूर्ण स्थितियाँ और वैचारिक भिन्नताएँ: स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। हालाँकि, इस नीति के कारण भारत-अमेरिका के बीच कई बार मतभेद उत्पन्न हुए, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौर में, जब अमेरिका ने सोवियत-विरोधी देशों को प्राथमिकता दी और भारत की तटस्थता को संदेह की दृष्टि से देखा। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिये अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ गठबंधन कर लिया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। 1970 का दशक- परमाणु तनाव और मतभेद: 1970 का दशक भारत-अमेरिका संबंधों के लिये निम्न बिंदु था, जिसका प्रमुख कारण भारत की परमाणु महत्त्वाकांक्षाएँ थीं। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे “स्माइलिंग बुद्धा” (Smiling Buddha) नाम दिया गया। इस परीक्षण से अमेरिका नाराज़ हो गया और उसने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के प्रावधानों के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा दिये। इसके अलावा, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को समर्थन तथा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उसकी भागीदारी ने और अधिक तनाव उत्पन्न किया। 1980 के दशक में मतभेदों के बावजूद संबंधों को स्थिर करने के प्रयास किये गए। 1982 में इंदिरा गांधी की अमेरिका की राजकीय यात्रा में व्यापार और परमाणु सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई। हालाँकि, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी और निरंतर परमाणु तनाव के कारण संबंध तनावग्रस्त रहे। 1990 का दशक – शीत युद्ध के बाद संबंधों का एक नया युग: शीत युद्ध की समाप्ति और 1991 में सोवियत संघ के पतन ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किये गए आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, जिससे यह वैश्विक बाज़ार, विशेषकर अमेरिका के साथ और अधिक एकीकृत हो गई। 1991 के खाड़ी युद्ध ने एशियाई क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत में अमेरिकी रुचि की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1998 में भारत द्वारा किये गए परमाणु परीक्षण (पोखरण द्वितीय) के कारण एक बार फिर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इन्हें अपेक्षाकृत शीघ्र ही हटा लिया गया। 2000 के दशक में भारत-अमेरिका संबंधों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया, विशेष रूप से 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद, जो दो दशकों में किसी पदस्थ अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। 2005 का अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस समझौते ने भारत के साथ परमाणु सहयोग पर 30 साल के अमेरिकी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी व परमाणु ऊर्जा एवं सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ावा दिया। 2010 – सामरिक और रक्षा संबंधों को मज़बूत करना: राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंध मज़बूत हुए, जिनमें रक्षा सहयोग, आतंकवाद-निरोधक नीतियां व आर्थिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।भारत-अमेरिका साझेदारी तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अर्द्धचालक और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग द्वारा परिभाषित हो रही है। वर्ष 2023 में शुरू की जाने वाली महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (ICET) इन संबंधों को मज़बूत करने, भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्रदान करने और दोनों देशों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अमेरिका और भारत ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में 825 मिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जो तकनीकी नेतृत्व में उनकी साझा रुचि को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में, अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। वर्ष 2024 में, दोनों देशों ने लघु और मध्यम उद्यमों (SME) पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये, जिसमें नवाचार और विकास का समर्थन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने में आपसी रुचि पर प्रकाश डाला गया। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग: जलवायु परिवर्तन एजेंडे में भारत और अमेरिका के बीच महत्त्वपूर्ण संरेखण (विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन व स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत) देखा गया है। हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच टकराव के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन लगातार विवाद का विषय रहा है। अमेरिका ने विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर उच्च टैरिफ और प्रतिबंधों के लिये भारत की नियमित रूप से आलोचना की है, जबकि भारत हाल के प्रशासनों के तहत अमेरिकी व्यापार प्रथाओं और संरक्षणवाद से निराश है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में अमेरिका ने भारत द्वारा अपने बाज़ारों में “न्यायसंगत और उचित पहुँच” प्रदान करने से इनकार करने का हवाला देते हुए भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज़ (GSP) के तहत दी जाने वाली प्राथमिकता प्राप्त व्यापार स्थिति समाप्त कर दिया था। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका के 28 उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगा दिये, जिससे व्यापारिक तनाव और अधिक बढ़ गया। ‘भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिये किसी ऐसे स्थान की खोज़ करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके।’ एक ओर ट्रम्प-मोदी की दोस्ती चर्चा में रही, वहीं अब दोनों देशों में शक-शोबा हो गया है। यह भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण है कि, डॉ. जयशंकर, विदेश मंत्री, विक्रम मिस्री, विदेश सचिव व पीएम कार्यालय, अपनी कूटनीति व डिप्लोमैटिक चर्चा द्वारा भारत-अमेरिका संबंधो को पुनः सकारात्मक राह पर लाये एक समय ‘हाउ-डी (how-d) मोदी कार्यक्रम’ व ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ के नारे लगाने वाले देशों में मतभेद आ गए हैं। अमेरिका के साथ भारत के सकारात्मक सम्बंध बनाये रखना महत्वपूर्ण चुनौति है।
प्रो. नीलम महाजन सिंह, (वरिष्ठ पत्रकार, सामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ, दूरदर्शन व्यक्तित्व व सालिसिटर)