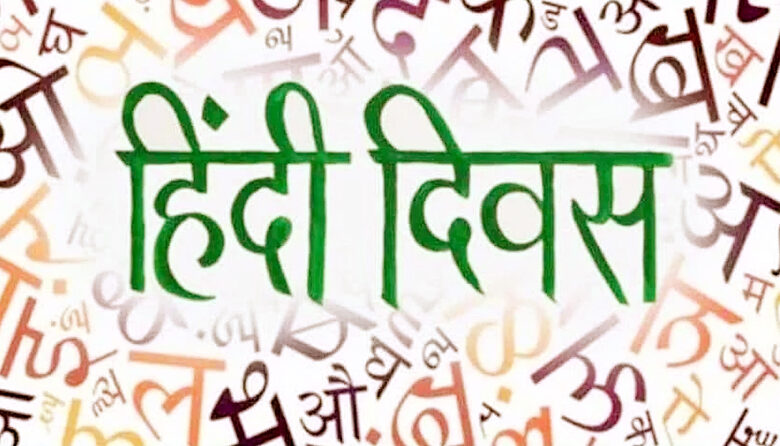
मुनीष भाटिया
आज़ादी के सात दशक बाद भी हिंदी को वह स्थान नहीं मिला, जिसकी अपेक्षा एक राष्ट्रभाषा से की जाती है। संविधान ने इसे राजभाषा अवश्य बनाया, किन्तु व्यवहार में अंग्रेज़ी का वर्चस्व हर क्षेत्र में दिखाई देता है। न्यायालयों, सरकारी कामकाज और निजी क्षेत्र में अंग्रेज़ी को सहज स्वीकार किया जाता है, जबकि हिंदी को लेकर कई राज्यों में विरोध देखा जाता है। यह विरोधाभास हमारी भाषाई व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं को नष्ट कर हिंदी को जबरन थोपा जाए, बल्कि प्रश्न यह है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ी को पूरे देश में एक वैकल्पिक भाषा के रूप में सर्वस्वीकार्य मान लिया गया है,उसी स्तर पर हिंदी को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता?
हिंदी के विरोध का अर्थ क्षेत्रीय भाषाओं को बचाना भर नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक स्वार्थ भी गहरे जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत और कुछ अन्य हिस्सों में हिंदी थोपने की आशंका ने इसे ‘राष्ट्रीय एकता की भाषा’ बनने से रोका। वहीं अंग्रेज़ी धीरे-धीरे शिक्षा, रोजगार और प्रशासन की भाषा बन गई। परिणामस्वरूप, हिंदी बोलने वालों की संख्या करोड़ों में होने के बावजूद इसे बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया।
आज की युवा पीढ़ी अंग्रेज़ी को सफलता की कुंजी मानती है क्योंकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हिंदी की उपस्थिति नगण्य है। जब तक नीतिगत स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में इसका सम्मान नहीं बढ़ सकता।
हालाँकि, डिजिटल जगत और सोशल मीडिया ने हिंदी को नई ऊर्जा दी है। फ़िल्म, साहित्य और पत्रकारिता में इसकी ताक़त स्पष्ट दिखती है। यदि सरकार और समाज मिलकर हिंदी को शिक्षा, प्रशासन और न्यायपालिका में समान अवसर दें, तो यह न केवल सम्मान पाएगी बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी सशक्त करेगी।
हिंदी को नई पीढ़ी के रोज़गार और शोध की भाषा बनाना होगा। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में हिंदी माध्यम को मज़बूत करना पड़ेगा। न्यायिक व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग से आम नागरिक को न्याय सुलभ हो सकेगा। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संतुलन बनाते हुए हिंदी को साझा पहचान का आधार बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी को गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपनाया जाए, तभी यह सचमुच राष्ट्र की भाषा बन पाएगी।







